रक्तपात के बीच ठिठका देश - मृणाल पांडे
रक्तपात के बीच ठिठका देश
मृणाल पांडे
दैनिक भास्कर
और अब, जबकि नक्सली दस्तों के हैबतनाक हौसले बुलंद हैं, कई चूजादिल विद्वान पोथे खोले बैठे हैं कि देश के संघीय ढांचे को चुनौती दिए बिना, सेना भेजे बिना, राज्य के स्वघोषित दुश्मनों के मानवाधिकारों का हनन किए बिना, स्थानीय जनजीवन में खलबली मचाए बिना, अगले चुनाव के संभावित घटक दल को खफा किए बिना कैसे इन हिंसक, अराजकता समर्थक गुरिल्ला जत्थों का जल्द और समूल विनाश हो! एक और छानबीन कमेटी बिठा दी गई है, जो छत्तीसगढ़ नरसंहार पर जब रपट देगी, तब देगी। जमीनी सच्चाई यह है कि अभी नक्सली वारदातें जारी हैं, पर चुनाव भी सर पर हैं। लिहाजा षड्यंत्र की अफवाहों में लिथड़ी समस्या की गेंद राजनीतिक दलों के बीच लतियाई जाने लगी है। गृहमंत्री तथा रक्षामंत्री की तरफ से मिले संकेतों के अनुसार नक्सली जत्थे भले बेगुनाह नागरिकों और सशस्त्र बलों के खून की नदियां बहाते रहें, अपने कैदियों को जेल तोड़कर उड़ा लें, स्कूल बंद करा दें, सड़क निर्माण रोक दें और जिलाधिकारियों का अपहरण कर फिरौती मांगें, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल उनसे अंतरराष्ट्रीय शांतिसेना की तरह पेश आते रहेंगे। समस्या का वाजिब हल नहीं खोजा गया इसलिए आज एकाधिक राज्यों (जिनमें छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, उड़ीसा, आंध्र तथा बिहार भी शामिल हैं) में सशस्त्र खेतिहरों, आदिवासी युवाओं को नक्सली हिंसक गुरिल्ला बना चुके हैं।
तीन दशक तक गठजोड़ सरकारों के तहत लगातार मौकापरस्त बनती गई राजनीति और उदारीकरण के तहत बनी अर्थनीति की असली जरूरतों के बीच आज एक बुनियादी और घातक विरोध नजर आता है। यानी सरकारें बनवाने और कायम रखने की राजनीतिक ताकत पूरी तरह क्षेत्रीय क्षत्रपों को मिल गई है, जिनके लिए क्षेत्रीय तथा पारिवारिक हित राष्ट्रीय हित से कहीं बड़े हैं; लेकिन आर्थिक नीतियों : जल, जंगल और जमीन के वितरण की अंतिम कुंजी केन्द्र सरकार के पास है। ऐसे में प्राथमिकता तय करना पेचीदा हो जाता है। खासकर विकास राशि तथा कुदरती संसाधनों का बंटवारा करने के मौके पर! यह देखकर कि विकास नीतियों को लागू कराने के केन्द्रीय फैसलों या गरीबी उन्मूलन प्रस्तावों के पारित होने से केन्द्र सरकार के शहरी और ग्रामीण वोटबैंकों की तुष्टि संभव है, हर विपक्षी गठजोड़ उन प्रस्तावों की आत्मा से सहमत होते हुए भी, संसदीय सत्रों को बार-बार ठप्प कराता है। इस लामबंदी की वजह से घरेलू टाटा हों या विदेशी पॉस्को जैसे विदेशी स्टील उत्पादक, उनको लाल कालीन से न्योतने के बाद भी न तो मनमोहन सिंह और न ही संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री उनको वादे के मुताबिक जमीन या खदान दिलवाते हैं।
फिर शहर बनाम गांव का चिरंतन द्वैत है। सबसे अधिक मतदाताओं वाले दो राज्य हैं : उत्तरप्रदेश और बिहार। उनके क्षत्रप तथा मतदाता गांवों का विकास पहले चाहते हैं और फैलते शहरी उद्योगों और शहरियों के लिए जंगलों, शामलात की जमीन या जलस्रोतों के बड़े आवंटन को, वह राज्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से कितना भी लाभकारी क्यों न हो, राजनीतिक वजहों से रोकते रहते हैं। उधर शहरों के फैलाव और बड़ी शहरी आबादी वाले दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र या झारखंड सरीखे राज्यों में इसका उलट है। शहरी वोटबैंकों का दबाव शहरी गरीबों और बिल्डरों उपक्रमियों को धन तथा जरूरी संसाधन देने और रोजगार सृजन पर है। लेकिन इससे संबंधित प्रस्ताव संसद या उसकी समितियों में पेश होते ही तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ, बिना यह सोचे कि कल उनकी सरकार बन भी गई तो यही भस्मासुर उनके पीछे पड़ जाएंगे, रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। गठजोड़ राजनीति के भीतरी दबावों के कारण पुलिसिया कार्रवाई पर राज्य और केन्द्र शायद ही कभी समवेत रणनीति बनाने पर राजी दिखते हों। उनके परस्पर आक्षेप आतंकी गुटों को मजबूती देते हैं तथा दुष्पीडि़तों को हर सरकार के खिलाफ लामबंद करना आसान बनाते हैं।
एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टि के अभाव में आज तक अशांत इलाकों में लोकतंत्र स्वतंत्र चयन का पर्याय नहीं बन पाया है। वहां आधुनिकता को, केन्द्र को गरियाने, स्थानीय संस्कृति के प्रतिगामी पक्ष को पोसने, लेकिन खुद भरपूर विदेश भ्रमण करने तथा आधुनिक जीवन जीने के शौकीन अधिनायकवादी नेतृत्व गरीब और अलग-थलग पड़ी जनता के बीच अपने लिए एक नैतिकता-निरपेक्ष अंध आस्था पैदा करते रहते हैं। इससे चुनावी जनाधार तो मजबूत होता है, लेकिन आतंकी गुटों पर समुचित कार्रवाई की घड़ी में हर राजनीतिक पार्टी अगर-मगर पर उतारू हो जाती है। जब छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश का अंग था, तब (1957 में) सामंतवाद विरोधी कांग्रेस भी बस्तर के विवादास्पद झक्की आदिवासी राजा प्रवीणचंद भंदेव से हाथ मिलाकर ही जीती। फिर झगड़ा होने पर (जो कि होना ही था) पहले 1961 में उनको नजरबंद किया गया और जब मार्च 1966 की मुठभेड़ में अनचाहे ही राजा मारे गए तो सत्ता में डैने फैलाने को आतुर विरोधी दल, यहां तक कि घोर सामंतवाद विरोधी कम्युनिस्ट दल भी राजा के पक्ष में सहानुभूति जताने बैठ गए। किसी ने नहीं कहा कि अगर सूबे में भिंड-मुरैना के डाकुओं पर गोली चलाना जायज माना गया, तो राज्य के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदिवासियों पर गोली चलाना क्या गलत था?
आतंकवाद के यह छुपे हितू क्या कृपा कर हमको बताएंगे कि बनने के लगभग डेढ़ दशक बाद भी अकूत वन तथा खनिज संपदा का मालिक छत्तीसगढ़ भारत के सबसे अधिक व्यक्तित्व हीन राज्यों में क्यों है? विषमता मिटानी थी तो अब तक उत्तराखंड, हिमाचल या हरियाणा की तरह राज्य का कोई आधुनिक तरक्कीपसंद सूबाई व्यक्तित्व क्यों नहीं बनाया गया? अपने इतिहास को खोए बिना राजस्थान तथा कर्नाटक आधुनिक उद्योग जगत से डोर जोड़ सकते हैं तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं? प्रांत के नेतृत्व और बस्तर की जनता, राज्य में आजादी के बाद से लगातार बाहर से आकर बसे और उसको आधुनिक उपक्रम और लोकतांत्रिक संस्थान देने वालों तथा मूल निवासियों की कोई साझा अखिल भारतीय पहचान, उनके बीच कोई सहज आत्मीयता आज भी क्यों गायब है? क्या कोई इस पर भी सोचेगा?
मृणाल पांडे
दैनिक भास्कर
और अब, जबकि नक्सली दस्तों के हैबतनाक हौसले बुलंद हैं, कई चूजादिल विद्वान पोथे खोले बैठे हैं कि देश के संघीय ढांचे को चुनौती दिए बिना, सेना भेजे बिना, राज्य के स्वघोषित दुश्मनों के मानवाधिकारों का हनन किए बिना, स्थानीय जनजीवन में खलबली मचाए बिना, अगले चुनाव के संभावित घटक दल को खफा किए बिना कैसे इन हिंसक, अराजकता समर्थक गुरिल्ला जत्थों का जल्द और समूल विनाश हो! एक और छानबीन कमेटी बिठा दी गई है, जो छत्तीसगढ़ नरसंहार पर जब रपट देगी, तब देगी। जमीनी सच्चाई यह है कि अभी नक्सली वारदातें जारी हैं, पर चुनाव भी सर पर हैं। लिहाजा षड्यंत्र की अफवाहों में लिथड़ी समस्या की गेंद राजनीतिक दलों के बीच लतियाई जाने लगी है। गृहमंत्री तथा रक्षामंत्री की तरफ से मिले संकेतों के अनुसार नक्सली जत्थे भले बेगुनाह नागरिकों और सशस्त्र बलों के खून की नदियां बहाते रहें, अपने कैदियों को जेल तोड़कर उड़ा लें, स्कूल बंद करा दें, सड़क निर्माण रोक दें और जिलाधिकारियों का अपहरण कर फिरौती मांगें, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल उनसे अंतरराष्ट्रीय शांतिसेना की तरह पेश आते रहेंगे। समस्या का वाजिब हल नहीं खोजा गया इसलिए आज एकाधिक राज्यों (जिनमें छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, उड़ीसा, आंध्र तथा बिहार भी शामिल हैं) में सशस्त्र खेतिहरों, आदिवासी युवाओं को नक्सली हिंसक गुरिल्ला बना चुके हैं।
तीन दशक तक गठजोड़ सरकारों के तहत लगातार मौकापरस्त बनती गई राजनीति और उदारीकरण के तहत बनी अर्थनीति की असली जरूरतों के बीच आज एक बुनियादी और घातक विरोध नजर आता है। यानी सरकारें बनवाने और कायम रखने की राजनीतिक ताकत पूरी तरह क्षेत्रीय क्षत्रपों को मिल गई है, जिनके लिए क्षेत्रीय तथा पारिवारिक हित राष्ट्रीय हित से कहीं बड़े हैं; लेकिन आर्थिक नीतियों : जल, जंगल और जमीन के वितरण की अंतिम कुंजी केन्द्र सरकार के पास है। ऐसे में प्राथमिकता तय करना पेचीदा हो जाता है। खासकर विकास राशि तथा कुदरती संसाधनों का बंटवारा करने के मौके पर! यह देखकर कि विकास नीतियों को लागू कराने के केन्द्रीय फैसलों या गरीबी उन्मूलन प्रस्तावों के पारित होने से केन्द्र सरकार के शहरी और ग्रामीण वोटबैंकों की तुष्टि संभव है, हर विपक्षी गठजोड़ उन प्रस्तावों की आत्मा से सहमत होते हुए भी, संसदीय सत्रों को बार-बार ठप्प कराता है। इस लामबंदी की वजह से घरेलू टाटा हों या विदेशी पॉस्को जैसे विदेशी स्टील उत्पादक, उनको लाल कालीन से न्योतने के बाद भी न तो मनमोहन सिंह और न ही संबद्ध राज्य के मुख्यमंत्री उनको वादे के मुताबिक जमीन या खदान दिलवाते हैं।
फिर शहर बनाम गांव का चिरंतन द्वैत है। सबसे अधिक मतदाताओं वाले दो राज्य हैं : उत्तरप्रदेश और बिहार। उनके क्षत्रप तथा मतदाता गांवों का विकास पहले चाहते हैं और फैलते शहरी उद्योगों और शहरियों के लिए जंगलों, शामलात की जमीन या जलस्रोतों के बड़े आवंटन को, वह राज्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से कितना भी लाभकारी क्यों न हो, राजनीतिक वजहों से रोकते रहते हैं। उधर शहरों के फैलाव और बड़ी शहरी आबादी वाले दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र या झारखंड सरीखे राज्यों में इसका उलट है। शहरी वोटबैंकों का दबाव शहरी गरीबों और बिल्डरों उपक्रमियों को धन तथा जरूरी संसाधन देने और रोजगार सृजन पर है। लेकिन इससे संबंधित प्रस्ताव संसद या उसकी समितियों में पेश होते ही तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ, बिना यह सोचे कि कल उनकी सरकार बन भी गई तो यही भस्मासुर उनके पीछे पड़ जाएंगे, रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। गठजोड़ राजनीति के भीतरी दबावों के कारण पुलिसिया कार्रवाई पर राज्य और केन्द्र शायद ही कभी समवेत रणनीति बनाने पर राजी दिखते हों। उनके परस्पर आक्षेप आतंकी गुटों को मजबूती देते हैं तथा दुष्पीडि़तों को हर सरकार के खिलाफ लामबंद करना आसान बनाते हैं।
एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टि के अभाव में आज तक अशांत इलाकों में लोकतंत्र स्वतंत्र चयन का पर्याय नहीं बन पाया है। वहां आधुनिकता को, केन्द्र को गरियाने, स्थानीय संस्कृति के प्रतिगामी पक्ष को पोसने, लेकिन खुद भरपूर विदेश भ्रमण करने तथा आधुनिक जीवन जीने के शौकीन अधिनायकवादी नेतृत्व गरीब और अलग-थलग पड़ी जनता के बीच अपने लिए एक नैतिकता-निरपेक्ष अंध आस्था पैदा करते रहते हैं। इससे चुनावी जनाधार तो मजबूत होता है, लेकिन आतंकी गुटों पर समुचित कार्रवाई की घड़ी में हर राजनीतिक पार्टी अगर-मगर पर उतारू हो जाती है। जब छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश का अंग था, तब (1957 में) सामंतवाद विरोधी कांग्रेस भी बस्तर के विवादास्पद झक्की आदिवासी राजा प्रवीणचंद भंदेव से हाथ मिलाकर ही जीती। फिर झगड़ा होने पर (जो कि होना ही था) पहले 1961 में उनको नजरबंद किया गया और जब मार्च 1966 की मुठभेड़ में अनचाहे ही राजा मारे गए तो सत्ता में डैने फैलाने को आतुर विरोधी दल, यहां तक कि घोर सामंतवाद विरोधी कम्युनिस्ट दल भी राजा के पक्ष में सहानुभूति जताने बैठ गए। किसी ने नहीं कहा कि अगर सूबे में भिंड-मुरैना के डाकुओं पर गोली चलाना जायज माना गया, तो राज्य के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदिवासियों पर गोली चलाना क्या गलत था?
आतंकवाद के यह छुपे हितू क्या कृपा कर हमको बताएंगे कि बनने के लगभग डेढ़ दशक बाद भी अकूत वन तथा खनिज संपदा का मालिक छत्तीसगढ़ भारत के सबसे अधिक व्यक्तित्व हीन राज्यों में क्यों है? विषमता मिटानी थी तो अब तक उत्तराखंड, हिमाचल या हरियाणा की तरह राज्य का कोई आधुनिक तरक्कीपसंद सूबाई व्यक्तित्व क्यों नहीं बनाया गया? अपने इतिहास को खोए बिना राजस्थान तथा कर्नाटक आधुनिक उद्योग जगत से डोर जोड़ सकते हैं तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं? प्रांत के नेतृत्व और बस्तर की जनता, राज्य में आजादी के बाद से लगातार बाहर से आकर बसे और उसको आधुनिक उपक्रम और लोकतांत्रिक संस्थान देने वालों तथा मूल निवासियों की कोई साझा अखिल भारतीय पहचान, उनके बीच कोई सहज आत्मीयता आज भी क्यों गायब है? क्या कोई इस पर भी सोचेगा?




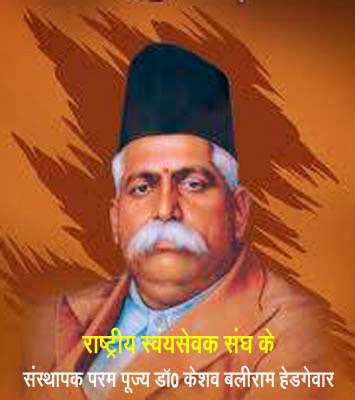


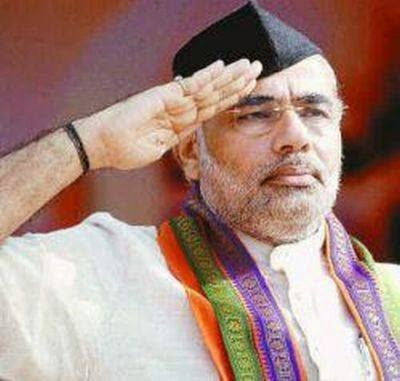
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें