सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ : गरीबी के आंकड़ों
http://www.livehindustan.com
गरीबी सिर्फ गरीबी नहीं है
बेशक, गरीबी एक गंभीर मामला है। गंभीर मामलों की दिक्कत यह होती है कि इन्हें लेकर या तो हम बहुत भावुक और जज्बाती हो जाते हैं, या शास्त्रीय किस्म के तर्कवादी बन जाते हैं, या फिर किसी इस या उस विचार के चलते समस्या से ही आंख मूंदने लगते हैं। गरीबी की दूसरी दिक्कत यह है कि इसके आकलन का सारा जिम्मा अर्थशास्त्रियों के हवाले होता है, उन्हें इसका आकलन अपने विषय की सीमा में उपलब्ध पैमानों से ही करना होता है। अर्थिक गणित के समीकरण गरीबी को आंकड़ों में बदल देते हैं और फिर आंकड़ों की तो फितरत ही अलग होती है। पहली समस्या यह आती है कि आंकड़ें चाहे जैसे भी हों, उनका आकार प्रकार चाहे कैसा भी हो वे अक्सर हमारी भावुकता और विचारधारा से मेल नहीं खाते। इसके अलावा खुद सांख्यिकीय के विद्वान ही यह कहते हैं कि अगर आपको सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ बोलना है तो आंकड़ों का सहारा लीजिए।
आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और उनकी व्याख्या से कईं तरह के खेल कर लेने की परंपरा भी पुरानी है। गरीबी के कम होने या न होने के आंकड़ों पर इन दिनों जो बहस चल रही है, वह कुछ इसी तरह का खेल भी है। वैसे आंकड़ों से अलग अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री एक बात पर सहमत दिखते हैं कि गरीब होने का अर्थ होता है वंचित होना। वे मानते हैं कि गरीबी सापेक्ष होती है। कहीं पर वह गरीब होता है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और कहीं पर वह गरीब होता है जिसके पास रहने को ठीक ठाक जगह नहीं होती। दूसरे शब्दों में गरीबी गैरबराबरी वाले समाज में सबसे निचली पायदान पर रहने वालों की आर्थिक स्थिति होती है। लेकिन किसी कल्याकारी राज्य में जब हम आर्थिक नीतियों से गरीबों के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो हमें आंकड़े ही चाहिए होते हैं। कितने लोग? कितने गरीब? कितनों को कितनी मदद दी जाए? वगैरह। इसी कोशिश में बनती है गरीबी की रेखा। यानी वह न्यूनतम आर्थिक स्थिति जिसके नीचे रहने वालों को तुरंत मदद की जरूरत है। इसका यह अर्थ कतई नहीं होता कि इसे रेखा के ऊपर रहने वाले अमीर हैं। गरीब तो वे भी हैं, लेकिन यह मान लिया जाता है कि उन्हें मदद की तत्काल उतनी जरूरत नहीं जितनी कि उससे निचली पायदान वालों को है।
इस गरीबी की रेखा को किस तरह तय किया जाए इसे लेकर अर्थशास्त्रियों में हमेशा मतभेद रहे हैं। पहले गरीबी को इससे नापा जाता था कि व्यक्ति को एक दिन में कितने कैलोरी भोजन मिलता है। लेकिन इसके खिलाफ तर्क यह था कि भोजन और कैलोरी को भुखमरी का पैमाना तो बनाया जा सकता है लेकिन आर्थिक गरीबी का पैमाना नहीं हो सकता। गरीब को भोजन ही नहीं दवा जैसी जरूरी चीजों पर भी पैसे खर्च करने होते हैं। इसी सोच के साथ यह तय किया गया कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना खर्च करता है इससे उसकी गरीबी नापी जाए। निसंदेह इस पैमाने में हेर फेर की पूरी गुंजाइश है। आप गरीबी के लिए तय दैनिक खर्च में दो चार रुपये घटा बढ़ाकर गरीबों की संख्या भी घटा बढ़ा सकते हैं। गरीबों की संख्या कम होने का ताजा विवाद भी इसी से जुड़ा है।
इस पैमाने की दिक्कत यह भी है कि मंहगाई जितनी तेजी से हर रोज बढ़ती है, उतनी तेजी से हम अपना खर्च सीमा वाला पैमाना नहीं बदल पाते। लेकिन सच तो यह है कि गरीबी के उन्मूलन में गरीबों की संख्या का सही आकलन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसके लिए क्या नीतियां अपनाई जा रही हैं। गरीबी के आंकड़ों को लेकर जितने मतभेद हैं, गरीबी उन्मूलन की नीतियों को लेकर उससे कईं गुना ज्यादा मतभेद हैं। सबसे बड़ा मतभेद वह है जो इन दिनों प्रोफेसर अमृत्य सेन और प्रोफेसर जगदीश भगवती की बहस के रूप में हमारे सामने है। अमृत्य सेन का मानना है कि गरीबी से लड़ने का सबसे अच्छा हथियार सरकार की कल्याणकारी नीतियां ही हो सकती हैं। यानी वैसी ही नीतियां जो इन दिनों रोजगार गारंटी और भोजन के अधिकार के रूप में चलाई जा रही हैं।
कल्याकारी नीतियों के कुछ समर्थक मानते हैं कि सीधे रोजगार और भोजन देने से ज्यादा जरूरी है कि सरकार उनमें क्षमता और दक्षता पैदा करे। शिक्षा का अधिकार इसी सोच का परिणाम है। दूसरी तरफ प्रोफेसर जगदीश भगवती और अरविंद पणिग्रियह जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है तेज आर्थिक विकास। उनकी राय है कि विकास बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर और आर्थिक खुशहाली धीरे धीरे सब तक पहुंचेगी। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। एक तीसरी सोच यह है कि तेज विकास और कल्याकारी नीतियां, दोनों ही चीजें एक साथ जरूरी हैं। अगर तेजी विकास होगा तो सरकार के पास कल्याणकारी नीतियों में लगाने के लिए ज्यादा संसाधन होंगे। मोटे तौर पर पिछले दो दशक से देश एक साथ इन दोनों को ही अपनाने की ओर बढ़ रहा है।
हालांकि वास्तविक हालात में गरीबी को सचमुच कम करना इस पूरी बहस से कहीं ज्यादा जटिल मामला है। कल्याणकारी नीतियों के बारे में अनुभव यह रहा है कि उन पर धन तो खर्च होता है लेकिन उसका वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता। बीच में ही कईं स्तरों का भ्रष्टाचार उस धन को सोख लेता है। यह व्यवस्था किसी की गरीबी नहीं हटाती, कुछ लोगों की अमीरी जरूर बढ़ा देती है। यह भी कहा जाता है कि अगर इन नीतियों को ईमानदारी से लागू कर दिया जाता तो शायद देश की गरीबी अभी तक खत्म हो चुकी होती। पिछले कुछ साल के तेज आर्थिक विकास में हम ट्रिकल डॉउन थ्योरी का हश्र भी देख चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब वित्तमंत्री थे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि भारत में ट्रिकल डॉउन इफेक्ट नाकाम साबित हुआ है।
गरीबी को लेकर इस समय भारत की जो समस्या है वह न तो गरीबी की रेखा का गलत आकलन है और न ही इसके लिए बनाई गई नीतियां हैं। समस्या का असली कारण गरीबी हटाने की राजनैतिक प्रतिबद्धता का न होना है। योजनाओं को लागू करने की जो प्रशासनिक व्यवस्था हमने बनाई है वही उसके लागू होने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। केंद्र और राज्यों में हम तकरीबन सभी दलों की सरकारें देख चुके हैं और किसी ने भी इस प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने या दुरुस्त करने में दिलचस्पी कभी नहीं दिखाई। ऐसे में आंकड़ें भी निर्थक हैं और उनकी कमी-बेशी पर होने वाली बहस भी।





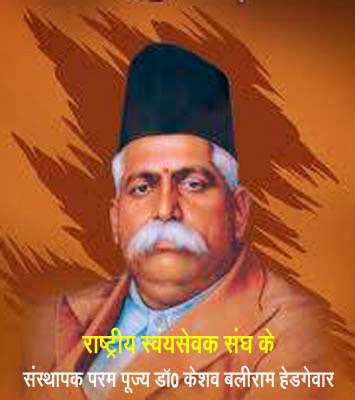

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें