भारत के मात्र 10-15 प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधियों नें बनाया था संविधान...?
विचार - भारत के संविधान निर्माण में कितनी जन भगदारी थी...?
---
1. भारत की प्रथम कार्यवाहक सरकार (Interim Government):
गठन: -
भारत की पहली अंतरिम सरकार 2 सितम्बर 1946 को गठित हुई थी।
किसने किया गठन:-
यह सरकार ब्रिटिश भारत में वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा गठित की गई थी, लेकिन इसमें भारतीय नेताओं को प्रमुख स्थान दिया गया।
नेतृत्व: -
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कार्यवाहक सरकार के उपाध्यक्ष (Vice President of the Executive Council) थे और वास्तविक रूप से सरकार का संचालन वही कर रहे थे।
उद्देश्य: यह सरकार ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था थी, जब तक कि पूर्ण स्वतंत्रता न मिल जाए और संविधान न बन जाए।
---
2. संविधान सभा का गठन:
गठन:-
संविधान सभा की स्थापना की योजना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी।
किसने किया गठन: -
इसका गठन ब्रिटिश सरकार ने ही किया था, परंतु इसके सदस्य भारतीय राज्यों और ब्रिटिश भारत से चुने गए थे।
पहली बैठक:-
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी।
महत्व: इस सभा ने भारत का संविधान तैयार किया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
---
3. अखंड भारत की दृष्टि:-
प्रारंभिक दृष्टिकोण: हाँ, 1946 में जब संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब भारत के विभाजन का निर्णय नहीं हुआ था। उस समय की योजना में अखंड भारत (हिंदुस्तान + पाकिस्तान + बांग्लादेश) को स्वतंत्र करना था।
बाद में विभाजन: लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अलग राष्ट्र (पाकिस्तान) की मांग और उपनिवेशीय तनावों के कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ।
---
सारांश:-
आपका कथन आंशिक रूप से सही है। अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था, परंतु उनका संचालन भारतीय नेताओं द्वारा हुआ। और प्रारंभ में यह भारत को एकजुट स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते देश का विभाजन हुआ।
----------=====------------
संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनमत (Direct Elections) के माध्यम से नहीं हुआ था, बल्कि यह परोक्ष निर्वाचन (Indirect Elections) द्वारा हुआ था। इसके लिए मतदाताओं की कुछ विशिष्ट अर्हताएँ (Qualifications) थीं, जो उस समय की ब्रिटिश प्रणाली और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार निर्धारित की गई थीं।
आइए विस्तार से समझते हैं:-
🧾 संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया:
कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अनुसार संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे।
ब्रिटिश भारत की प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे (यानि परोक्ष चुनाव)।
कुल 389 सीटें थीं (ब्रिटिश भारत और रियासतों सहित), लेकिन विभाजन के बाद 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में रहे।
---
🧑⚖️ मतदाताओं की अर्हताएँ (Qualifications of Electors):
जो लोग संविधान सभा के लिए सदस्य चुनने के लिए मत देने के पात्र थे, वे थे:
1. प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (Elected Members of Provincial Legislatures):
ये वे लोग थे जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुए 1937 के प्रांतीय चुनावों में चुने गए थे।
इन सदस्यों को ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार था।
2. मतदाताओं की अर्हताएँ (Who elected the provincial assemblies?):
1935 के अधिनियम के अनुसार, आम जनता को मताधिकार नहीं था।
केवल वे लोग वोट दे सकते थे जो निम्नलिखित योग्यता रखते थे:-
शिक्षा में न्यूनतम स्तर (जैसे मैट्रिकुलेट या अधिक),
संपत्ति का स्वामित्व (Property qualification),
आयकर भुगतान या नगरपालिका कर भुगतान करने वाले,
कोई पेशेवर स्थिति (जैसे वकील, डॉक्टर, ज़मींदार),
भारत की केवल लगभग 10-15% जनता को ही मतदान का अधिकार था।
🎯 निष्कर्ष:-
संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं, बल्कि परोक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था।
केवल प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही मतदाता थे।
और ये प्रांतीय सदस्य भी सीमित मताधिकार वाली प्रणाली से चुने गए थे, जहाँ सामान्य नागरिकों को बड़े पैमाने पर मतदान का अधिकार नहीं था।
---------=====--------
बिलकुल! नीचे भारत की संविधान सभा के गठन और उससे जुड़ी मतदाता अर्हताओं को एक टाइमलाइन (कालक्रम) के माध्यम से सरलता से समझाया गया है:
--
🕰️ भारत की संविधान सभा: गठन और निर्वाचन प्रक्रिया की टाइमलाइन
📅 1935 – भारत सरकार अधिनियम, 1935
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित।
इसके तहत भारत में प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था की गई।
प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराने का प्रावधान हुआ।
लेकिन वोट देने का अधिकार सीमित था – केवल कुछ शिक्षित, संपन्न, और करदाता वर्ग के लोगों को ही मतदान का अधिकार मिला।
📅 1937 – प्रांतीय चुनाव
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए।
इसी चुनाव से बने प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य बाद में संविधान सभा के लिए मतदाता बने।
---
📅 मार्च 1946 – कैबिनेट मिशन भारत आया
भारत में सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह मिशन भेजा।
इस मिशन ने संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की।
📅 जुलाई 1946 – संविधान सभा के चुनाव
प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्य चुने।
चुनाव परोक्ष (Indirect) थे – आम जनता नहीं बल्कि चुने गए विधायक ही मतदाता थे।
📅 9 दिसम्बर 1946 – संविधान सभा की पहली बैठक
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्षता की।
कुल चुने गए सदस्य: 389 (बाद में विभाजन के बाद 299 रह गए)
---
✅ मतदाताओं की अर्हताएँ (1937 के विधान सभा चुनावों के अनुसार):
अर्हता विवरण :-
🧑🎓 शिक्षा न्यूनतम शिक्षा स्तर (जैसे मैट्रिक या अधिक)
💰 संपत्ति कुछ मूल्य की संपत्ति या भूमि होनी चाहिए
🧾 करदाता आयकर, नगरपालिक कर आदि का भुगतान
👨⚖️ पेशा पेशेवर स्थिति – जैसे वकील, डॉक्टर, जमींदार
📌 नतीजा: भारत की केवल 10-15% जनता ही उस समय मतदान कर सकती थी।
🎯 महत्वपूर्ण तथ्य:-
संविधान सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत थी, लेकिन इसका संचालन भारतीय नेताओं ने किया।
भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) की शुरुआत 1951-52 के पहले आम चुनाव में हुई।
..........====........
हाँ, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में कितने लोगों को मतदान का अधिकार था। हालांकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) लागू नहीं था, फिर भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर यह संख्या लगभग ज्ञात है।
📊 1937 के चुनावों में मतदाताओं की संख्या:
🔹 भारत की कुल जनसंख्या (1931 की जनगणना के अनुसार):
लगभग 35 करोड़ (350 मिलियन)
🔹 योग्य मतदाता (Franchise Holders):
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार, केवल लगभग:
10% से 13% वयस्कों को ही मतदान का अधिकार था।
यह लगभग 3 से 4 करोड़ (30–40 मिलियन) मतदाता बनते हैं।
> 👉 ये मतदाता वही थे जिन्होंने 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान किया, और उन्हीं विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने।
🗳️ क्यों इतने कम लोग मतदाता थे?
1935 के अधिनियम ने मतदान के लिए कई सीमाएँ लगाई थीं:
अर्हता विवरण
📘 शिक्षा कम से कम प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा
🏠 संपत्ति जमीन या घर का स्वामित्व, किराया भुगतान
💼 पेशा वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि
💵 करदाता आयकर, संपत्ति कर, नगरपालिका कर का भुगतान
🧮 संक्षेप में आंकड़े:
विवरण अनुमानित संख्या
भारत की कुल जनसंख्या (1937) ~ 35 करोड़
वयस्क जनसंख्या ~ 20 करोड़
मतदान के पात्र लोग ~ 3 से 4 करोड़ (10-15%)
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ~ 1500+
संविधान सभा के चुने गए सदस्य 292 ब्रिटिश भारत से
🔎 निष्कर्ष:
1937 में, भारत की बहुसंख्यक जनता को मतदान का अधिकार नहीं था।
केवल विशेष अर्हताओं वाले लोग ही वोट डाल सकते थे।
इसी सीमित मतदाता वर्ग द्वारा चुनी गई विधानसभाओं ने 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का परोक्ष रूप से चयन किया।
------====--------
हाँ, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में कितने लोगों को मतदान का अधिकार था। हालांकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) लागू नहीं था, फिर भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर यह संख्या लगभग ज्ञात है।
📊 1937 के चुनावों में मतदाताओं की संख्या:
🔹 भारत की कुल जनसंख्या (1931 की जनगणना के अनुसार):
लगभग 35 करोड़ (350 मिलियन)
🔹 योग्य मतदाता (Franchise Holders):
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार, केवल लगभग:
10% से 13% वयस्कों को ही मतदान का अधिकार था।
यह लगभग 3 से 4 करोड़ (30–40 मिलियन) मतदाता बनते हैं।
> 👉 ये मतदाता वही थे जिन्होंने 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान किया, और उन्हीं विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने।
---
🗳️ क्यों इतने कम लोग मतदाता थे?
1935 के अधिनियम ने मतदान के लिए कई सीमाएँ लगाई थीं:
अर्हता विवरण
📘 शिक्षा कम से कम प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा
🏠 संपत्ति जमीन या घर का स्वामित्व, किराया भुगतान
💼 पेशा वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि
💵 करदाता आयकर, संपत्ति कर, नगरपालिका कर का भुगतान
🧮 संक्षेप में आंकड़े:
विवरण अनुमानित संख्या
भारत की कुल जनसंख्या (1937) ~ 35 करोड़
वयस्क जनसंख्या ~ 20 करोड़
मतदान के पात्र लोग ~ 3 से 4 करोड़ (10-15%)
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ~ 1500+
संविधान सभा के चुने गए सदस्य 292 ब्रिटिश भारत से
🔎 निष्कर्ष:
1937 में, भारत की बहुसंख्यक जनता को मतदान का अधिकार नहीं था।
केवल विशेष अर्हताओं वाले लोग ही वोट डाल सकते थे।
इसी सीमित मतदाता वर्ग द्वारा चुनी गई विधानसभाओं ने 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का परोक्ष रूप से चयन किया।
-------===---------
संविधान सभा में कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थीं, जिनमें से:
292 सदस्य — ब्रिटिश भारत की प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए (जैसा आपने कहा),
93 सदस्य — देशी रियासतों (Princely States) से आने थे,
4 सदस्य — मुख्य चीफ कमिशन्ड प्रदेशों (जैसे दिल्ली, अंडमान-निकोबार) से नामित होने थे।
अब आइए विस्तार से समझते हैं:
---
📊 संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों की संरचना (1946 में प्रस्तावित)
स्रोत सीटें चयन की विधि
🏛️ ब्रिटिश भारत की प्रांतीय विधानसभाएँ 292 परोक्ष चुनाव द्वारा (प्रांतीय विधायकों ने चुना)
👑 देशी रियासतें (Princely States) 93 नामांकन द्वारा – रियासतों के शासकों ने प्रतिनिधि भेजे
🏢 चीफ़ कमिशन्ड प्रदेश (Centrally Administered) 4 ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित
---
📅 बाद में क्या हुआ?
1. देश का विभाजन (1947):
भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के बहुत से सदस्य पाकिस्तान चले गए।
इसलिए:-
संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई।
इनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 70 सदस्य रियासतों से थे।
---
📌 रियासतों के प्रतिनिधि कैसे चुने गए थे?
देशी रियासतें (जैसे जोधपुर, हैदराबाद, कश्मीर, बड़ौदा आदि) ब्रिटिश भारत का औपचारिक हिस्सा नहीं थीं।
उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजें।
अधिकांश रियासतों ने बाद में भारत में विलय करके अपने प्रतिनिधि नामित किए — यह चयन नामांकन (Nomination) के माध्यम से हुआ, न कि चुनाव द्वारा।
🧾 निष्कर्ष:
सदस्य चयन की विधि स्रोत
292 परोक्ष चुनाव ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से
93 (बाद में 70) नामांकन देशी रियासतों द्वारा
4 नामांकन मुख्य कमिशन्ड क्षेत्रों से
👉 अत: केवल 292 सदस्य ही चुने गए थे, बाकी सभी नामित (Nominated) थे।
---------=====-------
देशी रियासतों (Princely States) से आए कई प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में सक्रिय भूमिका निभाई — हालांकि उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी, और शुरुआत में कई रियासतें अनिश्चित थीं कि वे संविधान सभा में भाग लें या नहीं। लेकिन जैसे-जैसे भारत का एकीकरण हुआ, उनकी भागीदारी बढ़ती गई।
---
🏰 देशी रियासतों की भूमिका: विस्तार से विश्लेषण
🔹 1. आरंभिक झिझक और अनिर्णय (1946-47):
1946 में जब संविधान सभा बनी, तब अधिकांश रियासतों ने शुरू में भाग नहीं लिया।
वे भारत सरकार से स्वतंत्र रहना चाहती थीं (जैसे हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़, कश्मीर आदि)।
ब्रिटिश नीति थी कि रियासतें चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं।
🔹 2. सरदार पटेल और माउंटबेटन की भूमिका:
सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन ने देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए अथक प्रयास किए।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (विलय पत्र) के ज़रिए अधिकतर रियासतें भारत में शामिल हो गईं।
🔹 3. नामांकित सदस्य संविधान सभा में पहुंचे (1947-48):
जैसे ही रियासतें भारत में शामिल हुईं, उन्होंने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे।
1947 के बाद से संविधान सभा में देशी रियासतों से लगभग 70 सदस्य सक्रिय रूप से जुड़े।
---
👤 कुछ प्रमुख रियासती प्रतिनिधि और उनकी भूमिका:
नाम रियासत भूमिका
नवाब इस्माइल अली खान पटियाला अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर योगदान
नरहरि विष्णु गाडगिल रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हुए योजना और प्रशासन पर बहस
महावीर त्यागी उत्तर प्रदेश लेकिन रियासती मुद्दों पर भी बोले
नवाब सर हमीदुल्ला खान भोपाल (शुरुआत में भाग नहीं लिया, बाद में विलय किया)
मीरा बेन (मदेलीन स्लेड) नामित सदस्य (रियासत नहीं, पर विशेष श्रेणी) – समाज सुधार पर योगदान
> ध्यान दें: कई प्रतिनिधियों ने विशिष्ट रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं किया लेकिन "रियासती क्षेत्र" का प्रतिनिधित्व करते थे।
🧾 उनकी भागीदारी के क्षेत्र:-
🔸 विलय और पुनर्गठन से जुड़ी संविधानिक व्यवस्थाएँ
🔸 अल्पसंख्यक अधिकार और रियासतों में उनके अधिकार
🔸 केंद्र-राज्य संबंध, क्योंकि रियासतों का एकीकरण एक चुनौती था
🔸 प्रशासनिक एकरूपता, क्योंकि हर रियासत का अपना कानून था
📌 मुख्य तथ्य: पहलू तथ्य
क्या रियासतों ने भाग लिया? हाँ, विलय के बाद
शुरुआत में झिझक क्यों थी? वे स्वतंत्र रहना चाहती थीं
कब शामिल हुईं? अधिकतर 1947 के बाद
क्या भूमिका निभाई? संविधान के प्रशासनिक ढाँचे, अल्पसंख्यक अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध आदि में
कुल प्रतिनिधि लगभग 70 रियासती प्रतिनिधि
---------====--------
हाँ, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में महत्त्वपूर्ण, विचारशील और सक्रिय योगदान दिया। आइए उनकी भूमिका पर विस्तार से नजर डालें:
---
🏛️ 1. प्रारंभिक प्रवेश और संवाद (अप्रैल 1947)
28 अप्रैल 1947 को पहली बार रियासती प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर सर बृजेन्द्रलाल मित्र (बारोडा) और के.एम. पन्निकार (बीकानेर) जैसे नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रियासतें भारतीय राष्ट्र की अभिन्न हिस्सा हैं और वे संविधान के निर्माण में बराबरी से योगदान देना चाहती हैं ।
> Sir Brojendra Lal Mitter:
“We, the States, are an integral part of India … we want to share the responsibility of framing the Constitution.”
---
📜 2. केंद्रीय नीति और विलय समझौते
सरदार पटेल व वी.पी. मेनन की पहल से Instrument of Accession के माध्यम से अधिकांश रियासतों ने भारत से विलय किया। इस प्रक्रिया को इतिहास में “masterstroke” कहा गया है ।
इस कदम से रियासती प्रतिनिधियों की संविधान सभा में भागीदारी औपचारिक और वैधानिक रूप से सुनिश्चित हुई।
---
🧩 3. राज्यों का प्रतिनिधित्व
रियासतों के करीब 70 सदस्य संविधान सभा में जुड़े, जिन्होंने केंद्र-राज्य संबंध, अल्पसंख्यकों के अधिकार, प्रादेशिक स्वायत्तता और संघीय ढाँचे जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बहुमूल्य इनपुट दिया ।
इनकी उपस्थिति ने संविधान सभा को भारत की “यूनिटी इन डाइवर्सिटी” (एकता में विविधता) की भावना से लैस किया।
---
👤 4. विशिष्ट रियासती प्रतिनिधियों के योगदान
1. **Lt. Col. Apji Dalel Singh (कोटा):**
कोटा राज्य के प्रतिनिधि, उन्होंने संविधान सभा में रियासती दृष्टिकोण से कई बहसों में भाग लिया।
उनके भाषणों में स्पष्ट दृष्टिकोण था कि रियासतों के अधिकारों की रक्षा, केंद्र-राज्य संतुलन और राजस्व नियंत्रण जैसे विषय प्राथमिकता से उठाए जाएँ ।
2. **Sir N. Gopalaswami Ayyangar (जम्मू-कश्मीर):**
जम्मू-कश्मीर के प्रधान मंत्री रहे, वे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हुए।
उन्होंने अनुच्छेद 370 की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जम्मू-कश्मीर को राज्य-विशेष दर्जा दिया ।
---
💡 5. रियासतों की बाध्यता व जुड़ाव
संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान “Privy Purse” (रियासतों को आर्थिक सहायता राशि) विषय भी प्रमुख रहा।
राज्य मंत्री (हालांकि नाम स्पष्ट नहीं है) ने उल्लेख किया कि प्राथमिक विलय की नींव उन रियासतों की राजीविलास और राज्य-हित की समझदारी का परिणाम थी ।
🧾 सारांश तालिका
पहलू भूमिका
🎤 प्रारंभिक भाषण रियासतों की कांग्रेस में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा (28 अप्रैल 1947)
🛡️ Instrument of Accession विलय और संविधान निर्माण में आधिकारिक भागीदारी एवं अधिकार
⚖️ नीति व अधिकार केंद्र-राज्य संबंध, अल्पसंख्यक हित, संघीय संतुलन
👥 प्रमुख प्रतिनिधि Apji Dalel Singh (कोटा), N.G. Ayyangar (ज&क)
💵 Privy Purse विषय विलय के दौरान आर्थिक व्यवस्था की स्थापना और समझौते
---
✳️ निष्कर्ष
देशी रियासतों ने संविधान सभा में:
अधिकारिक प्रवेश और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता में अपनी भागीदारी सिद्ध की।
Instrument of Accession और Privy Purse समझौतों के द्वारा अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की।
संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 370, प्रदेश-केन्द्र संबंध, अल्पसंख्यक सुरक्षा) में योगदान दिया।
------=------
भारत शासन अधिनियम और भारतीय संविधान में कितनी समानता है ... क्या भारत शासन अधिनियम का ही कुछ सुधरा रूप भारतीय संविधान है... विश्लेषत्मक आलेख
विश्लेषणात्मक आलेख: भारत शासन अधिनियम और भारतीय संविधान में समानता एवं अंतर
भारत का संविधान स्वतंत्र भारत का एक व्यापक एवं संप्रभु दस्तावेज़ है, जबकि भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा शासित भारत के लिए बनाया गया एक विधान था। कई विद्वानों का मत है कि भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम का "संशोधित और परिष्कृत रूप" है। यह कथन आंशिक रूप से सही है, परंतु संपूर्ण रूप से नहीं। इस आलेख में हम इन दोनों के बीच की समानताओं एवं असमानताओं का विश्लेषण करेंगे।
---
भारत शासन अधिनियम, 1935: संक्षिप्त परिचय
यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार लाना था। यह 1919 के अधिनियम की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और प्रभावशाली था। इसमें संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्तता, तथा केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का बँटवारा जैसे प्रावधान थे।
भारतीय संविधान और भारत शासन अधिनियम: समानताएँ
1. संघीय ढांचा (Federal Structure):
दोनों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा किया गया है। संविधान में अनुसूचियों के अनुसार तीन सूचियाँ (केन्द्रीय, राज्य और समवर्ती) दी गई हैं, जो अधिनियम 1935 की तीन सूचियों से प्रेरित हैं।
2. प्रशासनिक ढाँचा:
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की त्रैतीय प्रणाली दोनों में विद्यमान है। जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और विधानमंडल की व्यवस्था दोनों में है।
3. सरकारी पदों की संरचना:
राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ भारत शासन अधिनियम के गवर्नर जनरल की शक्तियों से मेल खाती हैं।
4. न्यायिक व्यवस्था:
उच्च न्यायालयों की स्थापना और उनके अधिकार, अधिनियम से प्रेरित हैं।
5. कानून निर्माण प्रक्रिया:
विधायिका द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम से काफी हद तक ली गई है।
6. संविधान की भाषा और प्रारूप:
संविधान का प्रारूप अंग्रेज़ी में तैयार किया गया, जो अधिनियम की भाषा और शैली से काफी प्रभावित था।
---
मुख्य भिन्नताएँ
1. स्वतंत्रता और संप्रभुता:
भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक क़ानून था, जबकि भारतीय संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया, और यह भारत की पूर्ण संप्रभुता को दर्शाता है।
2. नागरिकों के अधिकार:
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि भारत शासन अधिनियम में नागरिकों के लिए कोई मौलिक अधिकार सुनिश्चित नहीं किए गए थे।
3. गणराज्यात्मक स्वरूप:
भारत अब एक गणराज्य है, जहाँ राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) चुना जाता है, जबकि अधिनियम के समय ब्रिटिश सम्राट सर्वोच्च थे।
4. संविधान की लचीलापन और कठोरता:
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है, जबकि अधिनियम में कोई स्वदेशी संशोधन की व्यवस्था नहीं थी।
5. लोकतंत्र की स्थापना:
भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जबकि अधिनियम में मताधिकार सीमित था।
6. नवोन्मेष (Innovation):
भारतीय संविधान में DPSPs (राज्य के नीति निदेशक तत्व), पंचायती राज, और समाजवाद जैसे तत्व जोड़े गए हैं जो अधिनियम में नहीं थे।
---
निष्कर्ष
यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान ने भारत शासन अधिनियम, 1935 से संरचनात्मक प्रेरणा तो अवश्य ली, विशेषकर प्रशासनिक ढांचे के मामलों में, लेकिन यह मात्र एक संशोधित रूप नहीं है। भारतीय संविधान कहीं अधिक व्यापक, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और जन-केंद्रित दस्तावेज़ है। यह भारतीय परिस्थितियों, आदर्शों और स्वतंत्रता संग्राम की भावना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था।
इसलिए, भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान की प्रेरणा का स्रोत अवश्य रहा, परंतु संविधान की आत्मा, लक्ष्य और मूल तत्व पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
------===-------
भारत शासन अधिनियम, 1935 और भारतीय संविधान, 1950 के बीच धाराओं की प्रत्यक्ष मेल का कोई एक-से-एक तालमेल नहीं है, क्योंकि:
भारत शासन अधिनियम में धाराएँ (Sections) थीं।
जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद (Articles) होते हैं।
फिर भी, जब हम "कितनी धाराएँ मिलती हैं" पूछते हैं, तो आशय यह होता है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों की संरचना या विषयवस्तु भारत शासन अधिनियम की धाराओं से मिलती-जुलती है।
🔍 संरचनात्मक समानताओं की संख्या और उदाहरण:
भारतीय संविधान के प्रारूपण में भारत शासन अधिनियम, 1935 की लगभग 250 धाराओं में से लगभग 100 से अधिक धाराओं की भावना या संरचना किसी न किसी रूप में ली गई है।
उदाहरणस्वरूप कुछ प्रमुख समानताएँ:
भारत शासन अधिनियम, 1935 (धारा) भारतीय संविधान (अनुच्छेद) विषय
धारा 100–126 अनुच्छेद 52–78 संघ कार्यपालिका (राष्ट्रपति, मंत्री, PM)
धारा 232–236 अनुच्छेद 214–231 उच्च न्यायालय
धारा 45–46 अनुच्छेद 245–255 संसद की विधायी शक्ति
धारा 296–305 अनुच्छेद 294–300 संपत्ति, अनुबंध, उत्तरदायित्व
धारा 151 अनुच्छेद 148–151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
धारा 253–261 अनुच्छेद 268–293 वित्तीय संबंध
धारा 266 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएँ
धारा 321 अनुच्छेद 315–323 लोक सेवा आयोग
📌 महत्वपूर्ण तथ्य:
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्वयं यह स्वीकार किया कि संविधान का बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम, 1935 पर आधारित है।
बी. एन. राउ (Constitutional Advisor) और संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिनियम के कई प्रावधानों को मूलभूत परिवर्तन के साथ सम्मिलित किया।
✅ संक्षिप्त उत्तर (यदि परीक्षा के लिए चाहें):
> भारतीय संविधान के लगभग 250 से अधिक अनुच्छेदों में से करीब 100 से अधिक अनुच्छेदों की रूपरेखा और विषयवस्तु भारत शासन अधिनियम, 1935 की धाराओं से प्रभावित है। विशेष रूप से प्रशासनिक ढांचे, न्यायपालिका, वित्तीय संबंध, और लोक सेवा आयोग जैसे विषयों में स्पष्ट समानता पाई जाती है।
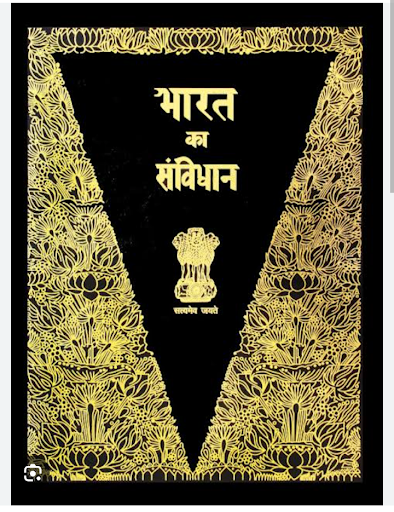



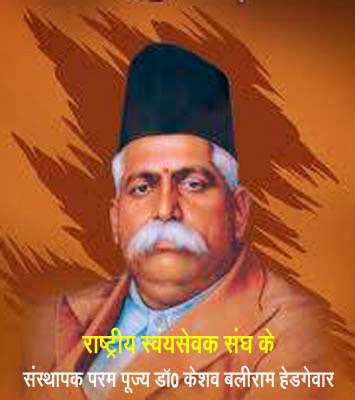


टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें