भारत के गौरवमय अतीत की एक झाँकी India's-glorious-past
- प्रस्तुतकर्ता - अरविन्द सिसौदिया 9414180151
आचार्य श्रीराम शर्मा के आर्शीवाद से.......
भारत के गौरवमय अतीत की एक झाँकी
समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान
(ज्ञान का अद्वितीय भण्डार युक्त उपरोक्त पुस्तक से )
मुद्रक : युगनिर्माण योजना, मथुरा। से साभार
Link :-
samast-vishwa-ko-bharat-ke-ajashra-anudan
आदर्श सहित उद्देश्य को यदि जीवन लक्ष्य बनाया जाए तो मनुष्य की अंत:चेतना अत्यंत बलिष्ठ होती जाती है और उस सामर्थ्य के कारण जीवनोपयोगी सभी आवश्यक सुविधा-साधन तो सहज में जुटते ही रहते हैं, साथ ही वे परिस्थितियाँ भी प्रस्तुत होती रहती हैं जिनके कारण आत्म संतोष मिलता रहे, आत्म गौरव उपलब्ध होता है रहे। आत्मबल ही इस संसार में सबसे बड़ा बल और वैभव है, इसे प्राप्त करने के उपरांत न कोई दुःख शेष रहता है और न अभाव, न दारिद्रय का कोई कारण शेष बचता है। अपने गुण-कर्म-स्वभाव की उत्कृष्टता यदि संपादित कर ली जाए तो भौतिक दृष्टि से तृप्तिदायक सुख और आनंददायक शांति की प्रचुर मात्रा सदैव सामने खड़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं श्रेय प्राप्त करते हैं और अपनी पीठ पर बिठाकर अनेकों को पार उतारते हैं। उनके चरणचिन्हों का अनुगमन करते हुए अनेकों अल्प-सामर्थ्यवान उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ने का प्रकाश एवं साहस प्राप्त करते हैं।
प्राचीन काल में संपत्ति का अर्थ होता था दैवी संपत्ति—गुण, कर्म, स्वभाव के व्यक्तिगत जीवन की उत्कृष्टता—व्यक्तित्व की प्रखरता। जिसके पास यह पूँजी थी, उसे संपत्तिवान कहा जाता था। उस समय प्रगति का अर्थ था—'अपनेपन' की परिधि को अधिकाधिक व्यापक, विस्तृत बनाना। आत्मीयता को शरीर और परिवार तक सीमित न रखकर उसे मनुष्यमात्र तक—प्राणिमात्र तक विस्तृत करना। दूसरों के दुःख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी रहना। अपनी चेतना तथा कर्त्तव्य से सुविस्तृत क्षेत्र को लाभान्वित करना। देश, धर्म, समाज और संस्कृति की—मानवता की परिपुष्टि के लिए बढ़े-चढ़े साहस और पुरुषार्थ का परिचय देना।
उन दिनों हर व्यक्ति सुसंपन्न बनना चाहता था, पर वह संपन्नता चाँदी के टुकड़ों, विलासिता के उपकरणों एवं ठाठ-बाट के अहंकारी प्रदर्शनों तक सीमित न थी। सामान्य लोगों की तुलना में कौन-कितने बड़े आदर्शवादी कीर्तिमान स्थापित कर सका, इसी कसौटी पर व्यक्ति का वर्चस्व परखा जाता था। जो महामानव की, भूसुर की भूमिका संपन्न करते थे, उन्हें ही संपत्तिशाली माना जाता था। लिप्सु-लोलुप, कृपण और कृतघ्न, संकीर्ण, स्वार्थी जहाँ-तहाँ उस जमाने में भी थे और उनके पास दूसरों की तुलना में वैभव भी अधिक रहता था, उससे शौक-मौज का लाभ भी उन्हें मिलता था, पर आत्म-संतोष और लोकमानस से सर्वथा वंचित वे अभागे निकृष्ट नरकीटों की तरह ही मौत के दिन पूरे करते थे। उन्हें विज्ञ समाज में कंगाल कहकर उपहासास्पद एवं घृणास्पद माना जाता था, भले ही अमीरी का ठाठ-बाट उनके पास कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो?
प्राचीन भारत का इतिहास इस देश में जन्मे नर रत्नों का इतिहास है। भारत-भूमि ने अन्न, वृक्ष, खनिज जैसी प्रकृति संपदाएँ उत्पन्न करके भौतिक संपदाओं के ही भंडार नहीं भरे, वरन देवमानवों का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया। घर-घर में नर रत्नों की खान थी। किसकी चमक कितनी प्रखर है, इसकी प्रतिस्पर्धा रहती थी। महानता की कसौटी पर किसका, कितना बढ़-चढ़ा मूल्यांकन होता है, इसी महत्त्वाकांक्षा से हर किसी का मन उद्वेलित रहता था। शूरवीर उन दिनों तलवार चलाने वाले ही नहीं माने जाते थे, वरन उन्हें भी योद्धा घोषित किया जाता था जिन्होंने अपनी पशु प्रवृत्तियों को, तृष्णा-वासना को, संकीर्ण स्वार्थपरता को पैरों तले रौंद सच्ची विजय प्राप्त की। ऐसे आत्मजयी योद्धा ही अभिनंदन और अभिवादन के पात्र समझे जाते थे। हर वर्ग में हर क्षेत्र में ऐसे आत्मजयी योद्धा भरे पड़े थे, उनके गौरवशाली अस्तित्व भारत माता की कीर्ति ध्वजा दसों दिशाओं में उड़ाते थे। इस आधार पर सुविकसित भारत की गौरव-गरिमा के सामने समस्त विश्व श्रद्धावनत मस्तक झुकाए खड़ा रहता था। उनकी विजय दुंदुभि विश्व के कोने-कोने में गूँजती, प्रतिध्वनित होती सुनाई पड़ती थी। प्राचीन इतिहास के जितने भी पृष्ठ पलटे जाएँ उनमें भारत की इसी विशिष्टता का उल्लेख स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ मिलता चला जाएगा।
उन दिनों अभिभावक यह प्रयत्न करते थे कि गर्भावस्था में पहुँचते ही बालक महामानवों की भूमिका में अवतरित हो। इसलिए उसकी शिक्षा उसी दिन से आरंभ हो जाती थी जिस दिन कि उसने गर्भ में प्रवेश किया। अर्जुन और सुभद्रा ने यही निश्चय किया था कि वे शूकर-कूकर की तरह ढेरों बच्चे नहीं जनेंगे। एक उत्पन्न करेंगे और उसे सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने आप को उस प्रकार का साँचा बनाएँगे जिससे उत्पन्न संतान महानता के साँचे में ढली हुई हो। वैसा ही हुआ भी। पति-पत्नी ने परस्पर संवाद और व्यवहार वीरोचित रखे, फलतः अभिमन्यु अभीष्ट विशेषता लेता आया। उसने उतना चक्रव्यूह आसानी से वेधन कर लिया जितना कि माता-पिता से गर्भावस्था में सीखा था।
मदालसा ने अपने कुछ बालकों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। जब तक वे बालक गर्भावस्था में रहे, तब तक उसने अपना चिंतन और चरित्र वैसा ही ढाला जैसी कि उसे संतान चाहिए थी। फलतः वे ब्रह्मवेत्ताओं के संस्कार लेकर जन्मे। एक बालक को उसने अपनी इच्छानुसार राज्य शासन कर सकने योग्य भी ढाला और वह भी ठीक उसकी इच्छानुसार जन्मा।
कुंती को देव गुणों से सुसज्जित संतान की आवश्यकता थी। उसने देव तत्त्वों से अपना रोम-रोम ओत-प्रोत किया और जिस-जिस दैवी शक्ति से सुसज्जित बालक की आकांक्षा की, ठीक उसी स्तर के उत्पन्न किए। सूर्यगुण संपन्न—कर्ण, इंद्र पुत्र—अर्जुन, धर्मराज पुत्र—युधिष्ठिर, पवनपुत्र—भीम, अश्विनीकुमार से—नकुल, सहदेव उत्पन्न माने जाते हैं। यह विद्या उन दिनों घर-घर में ज्ञात थी। सभी जानते थे कि अभिभावकों की आकांक्षा, निष्ठा और क्रिया जिस स्तर की होगी, वैसे ही बालक जन्मेंगे। इसलिए बच्चों का शिक्षण अभिभावक आत्मनिर्माण के रूप में आरंभ करते थे।
अंजनी को जैसा बालक अभीष्ट था वैसी उसने गर्भावस्था में तैयारी की। "राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम" वाली क्षमता को लेकर हनुमान जन्मे। वे वज्र-अंगी (वजरंगी) अनायास ही नहीं थे। माता की महत्त्वाकांक्षा के अनुरूप ही यह निर्माण संभव हुआ था।
राम चाहते थे कि उनके बालक विशिष्ट महानता से ओतप्रोत हों। राजमहल का वातावरण इसके लिए अनुकूल न था, तो उन्होंने सीता को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा, ताकि गर्भावस्था में माता को भ्रूण के उपयुक्त वातावरण में रहने का अवसर मिले। लव-कुश जन्मे तो वे ठीक वैसे ही थे, जैसा कि उनके अभिभावकों ने चाहा।
शकुंतला कंव ऋषि के आश्रम में पली थी। उसके पेट में दुष्यंत का गर्भ आया तो उसने यही चाहा कि संतान अपने देश का मुख उज्ज्वल करे। फलतः सिंह-शावकों से खेलने वाला भरत उसकी कोख से जन्मा और उस महाप्रतापी के पुरुषार्थ ने उसी के नाम पर इस पूरे देश का नामकरण 'भारतवर्ष' के रूप में कर दिया।
नचिकेता के उदारचेता पिता वाजिस्रवा जब समस्त धन-धान्य लोकमंगल के लिए दान दे चुके तो उसने पूछा—आप लोभ त्याग की परीक्षा में सफल हो चुके, फिर मोह त्याग में क्यों असफल होते हैं, मुझे खिलौना बनाकर क्यों अपने पास रखना चाहते हैं, लोक-मंगल के लिए मुझे भी दान क्यों नहीं दे देते? वाजिस्रवा ने पुत्र को अपने से बढ़कर आदर्शवादी देखा तो हर्षोल्लास से उनकी आँखें डबडबा आईं। उन्होंने तत्काल महा तपस्वी यमाचार्य के हाथ में अपने पुत्र नचिकेता का हाथ सौंप दिया और ब्रह्मवेत्ता बनकर इस विश्ववसुधा का गौरव बढ़ाने में समर्थ हुआ।
आद्य शंकराचार्य की माता अपने इकलौते पुत्र को भौतिक प्रगति में सुख-समृद्धि युक्त देखना चाहती थी। पुत्रवधू और पौत्र के साथ रहने को लालायित थी। माता की मोह-ममता को उसके दस वर्षीय बालक ने चतुरतापूर्वक तोड़-मोड़कर फेंक दिया। प्रसिद्ध है कि उन्हें नदी नहाने के समय 'मगर ने पकड़ा' तो चिल्ला करके बोले कि मुझे शंकरजी को दान करो अन्यथा मगर खा जाएगा। माता ने अपना बालक शिवजी को दान कर दिया। वे मगर के मुँह में से छूटकर बाहर आ गए और परिव्राजक बनकर भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने में समर्थ हुए।
ध्रुव ने माता के मोह को निरस्त किया और तप साधना में संलग्न होकर ध्रुवतारा के रूप में ब्रह्मांड को अपनी कक्षा में घुमाने वाले केंद्र बिंदु बने। प्रहलाद छोटा बालक तो था पर उसे मोह-ग्रस्त पिता का वह आदेश-आग्रह स्वीकार न हुआ जिसके अनुसार नीति-अनीति का ध्यान न करके अधिक से अधिक वैभव-उपार्जन के लिए समझाया जाता था।
समर्थ गुरु रामदास के घरवाले उन्हें विवाह के बंधन में बाँधकर सामान्य प्राणियों की तरह जीने के लिए विवश कर रहे थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि विवाह वेदी पर वधू को बिठा दिया गया। उनकी अंतरात्मा ने पुकारा कि इंद्रिय तृप्ति का पशु-प्रयोजन करते हुए मानव जीवन को व्यर्थ न कर, अपनी दिव्य क्षमताओं को स्त्री-बच्चों के छोटे दायरे में खरच न कर, उसे विश्व वसुधा की संपदा बना। अंतरात्मा की पुकार उन्होंने सुनी और विवाह वेदी पर से उठकर ताबड़तोड़ भाग खड़े हुए। वेदी की अवज्ञा जरूर हुई, पर उनका फैसला भी धर्म की परिधि से बाहर नहीं था। मोह ग्रस्तों का मोह तोड़ देना भी तो एक धर्म ही है। बड़े-बूढ़े क्षोभ व्यक्त करते रहे पर समर्थ गुरु रामदास वह करने में समर्थ हुए जो सौ जन्मों तक विवाह और संतानोत्पादन करते रहने पर भी नहीं कर सकते थे।
दशरथ भी कुछ ऐसा ही परामर्श राम को दे रहे थे कि वरदान कैकेयी को दिया है, तुम्हें वन जाने का आदेश नहीं दिया। झूठा पड़ूँगा, तो कैकेयी के सामने मैं पड़ूँगा। तुम वन मत जाओ? राम ने उनका मोह तोड़ा और कहा कि संतान-सुख बड़ा नहीं है, कर्तव्य बड़ा है।
कृष्ण ने भी गोपियों का और अपनी दोनों माताओं का मोह तोड़कर व्रज को छोड़ा था। उन्होंने सभी स्वजनों और प्रेमियों को समझाया कि जो उच्च कर्तव्यों में बाधा पहुँचाए वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह के बंधन तोड़ने में अधर्म नहीं है। यह कह कर कृष्ण व्रज का परित्याग करके कर्त्तव्य की पुकार पूरी करने के लिए, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने की तैयारी करने के लिए अन्यत्र चले गए। तब वे किशोरावस्था में पदार्पण ही कर रहे थे।
गुरु गोविंदसिंह के बालकों के सामने जीवित रहने के लिए इस्लाम स्वीकार करने की शर्त थी, बच्चों ने हँसते-हँसते जीवित दीवार में चुने जाने की दुरूह पीड़ा सहकर अपने प्राण गँवाए। वे जानते थे कि जीवन-मरण का कोई महत्त्व नहीं। सर्वोपरि महत्ता आदर्शों की रक्षा करना है।
कुंती अज्ञातवास की अवधि में अपने बालकों को लेकर एक ब्राह्मण परिवार में छिपी हुई दिन काट रही थी। उस गाँव में हर घर से एक मनुष्य राक्षस के द्वारा खाए जाने का क्रम चल रहा था। उस दिन आश्रयदाता ब्राह्मण के इकलौते पुत्र की बारी आ गई। पाँचों बच्चे मचल पड़े। हममें से एक राक्षस के सामने क्यों न चला जाए? और ब्राह्मण बालक को क्यों न बचा लिया जाए? उनके प्रबल आग्रह ने कुंती को बात मानने के लिए बाध्य कर दिया। अब इस सौभाग्य का लाभ कौन उठाए? इस बात पर सब बच्चे आपस में लड़ने लगे। अंतत: गोली निकालकर भाग्य का फैसला कराया गया। निर्णय भीम के पक्ष में हुआ। वह राक्षस के सामने हँसता-उछलता चला गया और स्वयं शिकार बनने के स्थान पर उलटा उसे ही मारकर आया। बच्चे उन दिनों जानते थे कि मरना भी यदि सदुउद्देश्य के लिए संभव हो सके तो वह हजार बार जीने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर है।
विवाह आदर्शों की स्थापना के लिए दो आत्माओं के मिलन के रूप में होते थे, कामुकता के घृणित प्रयोजन की पूर्ति के लिए नहीं। दोनों मिलकर परिवार को एक छोटे आदर्श राष्ट्र के रूप में विकसित करते थे। परिवारों की संरचना एक सुव्यवस्थित समाज संरचना की प्रयोगशाला के रूप में होती थी। इस पर पति-पत्नी न्यूनतम संतानोत्पादन करते थे। बच्चों को सुसंस्कृत बनाने पर ध्यान देते थे। विवाहित होने पर भी संतानोत्पादन थोड़े ही करते थे। जो करते थे उनके सामने विशेष लक्ष्य रहता था। वासनात्मक उन्माद उन्हें इसके लिए प्रेरित नहीं करता था। यह आदर्श न केवल ऋषियों वरन सामान्य स्तर के लोगों में भी प्रचलित था।
गृहस्थ जीवन में भी जनसाधारण के बीच आदर्शों की घोर प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता ठनी रहती थी। कौन किससे आगे निकलता है यह चुनौती अपने-अपने क्षेत्र में हर कोई अपने साथियों को देता रहता था। राम और भरत दोनों के सामने ऐसा ही धर्म संकट उत्पन्न था। दोनों ही चाहते थे कि त्याग और आदर्श के क्षेत्र में उनकी हेठी न होने पाए। 'राज्य हमें नहीं दूसरे को मिले' इस प्रतिद्वंदिता में कोई हारा नहीं। फैसला यह हुआ कि राम की तरह ही भरत भी चौदह वर्ष तक तपस्वी जीवन जीयेंगे। राज सिंहासन पर राम की खड़ाऊँ स्थापित की जाएँगी।
विश्वामित्र उन दिनों नवयुग का सूत्रपात कर रहे थे, उन्हें साधनों की आवश्यकता थी। उनके शिष्य हरिश्चंद्र ने पूर्ण निस्पृहता का परिचय दिया। अपनी सारी संपदा ऋषि के हवाले कर दी। कमी पड़ी तो अपने को, स्त्री-बच्चों को बेचकर प्रस्तुत आवश्यकता की पूर्ति करने का आदर्श प्रस्तुत किया। सुदामा के गुरुकुल की अभावग्रस्त स्थिति दूर करने के लिए कृष्ण ने अपनी द्वारिका की अधिकांश संपत्ति का अधिकांश भाग ऋषि सुदामा को सौंप दिया था। राजा कर्ण को विपुल वेतन मिलता था, वे अपनी दैनिक आय में से अपने निर्वाह की न्यूनतम राशि लेकर शेष उसी दिन सत्प्रयोजनों के लिए दान कर देते थे। मरते समय दाँतों में लगा सोना तक दान कर जाने वाले कर्ण की परम्परा उन दिनों सभी सुसंपन्न व्यक्तियों में प्रचलित थी। कभी किसी के पास धन जमा हो भी गया तो विशिष्ट अवसर सामने आते ही उसने भामाशाह की तरह अपनी सारी संपदा प्रताप जैसे प्रयोजनों के लिए सौंपते हुए अपना भार हलका कर लिया।
राजा जनक व्यक्तिगत निर्वाह के लिए कृषि करते थे और स्वयं हल चलाते थे। राज्यकोष प्रजा की अमानत था और उसी के लिए खरच होता था। ऐसा ही आचरण अन्य राजा भी करते थे। रानी अहिल्या बाई के राज्यकोष में से अधिकांश धर्म प्रयोजनों के लिए खरच होता रहा। राजनीतिक विकृतियों का निवारण करने के लिए प्रस्तुत अश्वमेध योजनाएँ और सामाजिक अव्यवस्थाओं का निराकरण करने के लिए प्रस्तुत वाजपेय यज्ञ अभियानों में न केवल राजाओं के राज्यकोष खाली होते थे, वरन संपन्न लोगों की संपन्नता भी झाड़-बुहारकर साफ कर दी जाती थी।
उन दिनों लोकमंगल के प्रयोजनों में निरत साधु संस्था के सदस्य—साधु और ब्राह्मण अपने आप में एक पवित्र संस्था होते थे। परमार्थ जीवन जीते थे, उन्हें जनता मुक्तहस्त से दान देती थी। कब किस प्रयोजन लिए कितना धन खरचा किया जाए यह निर्णय उन ऋषि कल्प महामानवों को ही सौंप दिया जाता था और ब्रह्मभोज तथा दान-दक्षिणा के रूप में वे देव पुरुष पर्याप्त साधन-सामग्री प्राप्त कर लेते थे। फलस्वरूप लोकमंगल की विभिन्न प्रवृत्तियाँ सहज ही फलती-फूलती रहती थीं। प्रत्येक हर्ष एवं पर्व के अवसर पर दानपुण्य की आवश्यकता हर गृहस्थ में समझी जाती थी। गृहस्थों की दान प्रवृत्ति विभिन्न कर्मकाण्डों एवं धर्मायोजनों के माध्यम से उठती-उभरती रहती थी। फलतः समाज में इन प्रवृत्तियों को ऊँचा उठाने वाले क्रिया-कलाप इतने बड़े-चढ़े रहते थे कि न केवल अपना देश वरन समस्त विश्व उस दान-पुण्य की जनभावना से समुचित लाभ उठाता रहता था।
मंदिर उन दिनों देव प्रतिमा पूजन भर तक की रूढ़ियाँ पूरी नहीं करते थे। उन दिनों के समस्त देवालय अपने क्षेत्र में आदर्शवादी प्रेरणाओं का आलोक फैलाने वाले सफल केंद्र बिंदु बनकर अनेकानेक रचनात्मक धर्म प्रवृत्तियों का संचालन करते थे। कोई मंदिर देवालय अभावग्रस्त नहीं रहता था और उपलब्ध साधनों को मंदिरों का संचालन-कर्ता पुरोहित पूरी तरह जन-कल्याण में ही प्रयुक्त करता था? गृहस्थ अपना घर परिवार तो चलाते ही थे पर साधु-ब्राह्मणों द्वारा संचालित धर्म प्रयोजनों में कहीं कुछ भी कमी न पड़ने पाए इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। व्यक्तिगत वैभव वृद्धि के स्थान पर धर्म प्रयोजनों के लिए कुछ अधिक रखने की प्रवृत्ति हर साधन-संपन्न मनुष्य के मन में निरंतर उफनती रहती थी।
इन परिस्थितियों जैसा इस देश का प्रत्येक नागरिक आदर्शवादिता की प्रतिमूर्ति था। हर भारतीय का चरित्र एक महामानव का चरित्र था। उनमें से कभी-कभी कोई दृष्टांत, उदाहरण चर्चा का विषय भी बनते रहे हैं, पर जब सभी लोग उस स्तर के थे तो चर्चा भी आखिर कहाँ तक की जाए?
अभिभावकों के प्रति संतान के कर्त्तव्यों के उदाहरण ढूँढें तो श्रवणकुमार द्वारा अंधे माँ-बाप को कंधे पर काँवर में बिठाकर तीर्थयात्रा कराना, भीष्म पितामह का अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन अविवाहित रहना, ययाति पुत्र का अपना यौवन वृद्ध पिता को देना, सत्यवान का तपस्वी पिता की सेवा व्यवस्था लकड़हारा बनकर करते रहना यह सिद्ध करते है कि उन दिनों के सामान्य से सामान्य संतान को कर्तव्यपरायणता के स्तर तक पहुँचा हुआ पाया जाएगा।
पतिव्रत धर्म निर्वाह करने वाली सावित्री, दमयंती, सीता, गांधारी सर्वत्र मिलेंगी। स्वयं कष्टमय जीवन स्वीकार करके, पतियों को कर्तव्य पथ पर धकेलने वाली वीर नारियाँ घर-घर में मौजूद थीं। वे उन्हें नीचे नहीं गिराती थीं वरन ऊँचा उठाती थीं। पुत्रों को गुरुकुल के लिए, पतियों को धर्मयुद्ध के लिए भेजते हुए वे मोहग्रस्तता के आँसू नहीं बहाती थीं वरन गर्व-गौरव के साथ आरती उतारते हुए विदा करती थीं। हाड़ा की रानी की तरह उन्हें अपना सिर काटकर पति को मोहग्रस्तता से उबारने में आपत्ति नहीं होती थी। पन्नादाई को अपना बच्चा प्यारा तो था, पर सौंपे हुए कर्त्तव्य से अधिक नहीं। उसने स्वामी का बच्चा बचाने के लिए अपने लाड़ले की आहुति चढ़ाते हुए आघात तो सहा पर मन यह सोचकर हलका कर लिया कि उसने नारी की गरिमा की एक उपयुक्त स्थापना करने में गौरवमयी परंपरा सही रूप में निभाई। चित्तौड़ की रानियों ने अपना शरीर नहीं, नारी का साहस जीवित रखना उचित समझा और वे जीवित जलने जैसे कष्ट को सहने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो गईं।
विवाह हर लड़की के लिए न तो आवश्यक है और न अनिवार्य, यदि किसी में लोक-कल्याण के लिए कुछ कर गुजरने का साहस हो तो उसे अविवाहित रहकर अपनी शक्तियों का पूर्ण समर्पण लोकमंगल के लिए करना चाहिए। इसके अगणित उदाहरण प्राचीन इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं। मनु-पुत्री इला ने ब्रह्मवादिनी का आदर्श निभाया और वे ब्रह्मवेत्ताओं में अग्रणी थीं। ऋग्वेद में घोसा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, जुहू, अदिति, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, शाश्वती, सूर्या आदि ब्रह्मवादिनी महिलाओं का वर्णन मिलता है।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में सीता और सावित्री नामक दो ब्रह्मवादिनियों का वर्णन है। सिद्धा, सुलभा, शिवा, श्रीव्रती, स्वधा, वपुना आदि कितनी ही कन्याएँ ऐसी हुई हैं जिन्होंने गृहस्थ में प्रवेश करने की अपेक्षा पुरुष ऋषियों की भाँति लोकमंगल के लिए अपना जीवन समर्पित किया और यह सिद्ध किया कि नारी के लिए विवाहित होना कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। वह पुरुष की तरह ही इच्छा और रुचि का विषय रहा है।
भारत की समुन्नत परिस्थिति और परिष्कृत मन:स्थिति का श्रेय यहाँ के ऋषियों को दिया जाता है। यह उचित भी है। उज्ज्वल चरित्र, उत्कृष्ट चिंतन और साहसिक पुरुषार्थ का त्रिविध समन्वय जिन व्यक्तियों में होगा वे स्वयं तो ऊँचे उठेंगे ही, अपने साथ-साथ लोकमानस को और समस्त वातावरण को भी ऊँचा उठाएँगे। ऋषियों की क्रिया-प्रक्रिया यही थी। वे सार्वजनिक क्षेत्र के हर पक्ष को देखते और सँभालते थे। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, परशुराम जैसे ऋषि धनुर्वेद में पारंगत थे। ये शस्त्र निर्माण और संचालन की शोध एवं शिक्षा के कार्य में संलग्न थे, ताकि असुरता से सफलतापूर्वक जूझा जा सके। चरक, सुश्रुत, वागभट्ट, अश्विनी कुमार, धन्वंतरि जैसे ऋषि स्वास्थ्य संबंधित और चिकित्सा के रहस्यों को ढूँढ़ने और उन्हें सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत करने में संलग्न थे। नागार्जुन, हारीत और सुषेन जैसे ऋषि रसायन विद्या के विकास और विस्तार में जुटे हुए थे। विश्वकर्मा, शतोधन जैसे ऋषियों ने शिल्प एवं वास्तुकला के संबंध में जो खोजा उससे विश्व सौंदर्य में असाधारण वृद्धि हुई। नारद, उपमन्यु, उद्दालक जैसे ऋषि स्वर शास्त्र के सामगान में पारंगत थे। उन्होंने गान-वाद्य की कला के मर्मों से जन मानस को आंदोलित किया और उसके रसास्वादन का विधि-विधान समझाया।
उत्कच, विद्रुध, महानंद जैसे ऋषि कृषि और पशुपालन का विज्ञान विकसित करने में जुटे थे। व्यास परंपरा के ऋषियों ने शास्त्र रचना की मुहिम सँभाली। सूत परंपरा के ऋषि प्रवचनकर्ता थे। चाणक्य, याज्ञवल्क्य, कंव, धौम्य जैसे ऋषियों द्वारा विश्व विद्यालय स्तर के शिक्षा संस्थान चलाए जाते थे। छोटे-बड़े गुरुकुल तो प्रायः सभी ऋषि चलाते थे। कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि जैसे दार्शनिकों द्वारा विश्वमानव की बौद्धिक क्षुधा बुझाने के लिए बहुमूल्य प्रतिपादन किए जाते रहे। वसिष्ठ, शुक्राचार्य, विदुर आदि ऋषि राजतंत्र का मार्गदर्शन करने में निरत थे। च्यवन, दधीचि आदि ऋषियों ने तप साधना करके मानवी अंत:स्थल में छिपी रहस्यमय शक्तियों के उपयोग का पथ प्रशस्त किया था। लोकमंगल के अनेकानेक प्रयोजनों में यह ऋषि वर्ग के लोग निरंतर संलग्न रहते थे।
अनीतिपूर्ण प्रतिबंधों को धर्म-मर्यादा का नाम जब भी दिया गया तब तुरंत उसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया गया। बड़े भाई की आज्ञा छोटे भाई को माननी चाहिए—इस मोटे अनुशासन के नियम के साथ जब अनीति को जोड़ा गया तो विभीषण ने अपने बड़े भाई का परामर्श मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। हिरण्यकशिपु पिता तो था, पर वह जो कहता था अनीतिमूलक था। प्रहलाद उसके विरुद्ध तनकर खड़ा हो गया और अंत तक विरोध पर डटा रहा। भरत ने माता का कहना न मानकर राज लेने के आदेश को स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की अवज्ञा करके वामन को दान देने का साहस दिखाया। एक ओर जहाँ धर्म अनुशासन पालन के लिए भारतीय संस्कृति में निर्देश हैं, वहाँ यह छूट भी पूरी तरह दी गई है कि यदि स्वजन अथवा बड़े कहे जाने वाले लोग भी अनीति के लिए बाध्य करें तो स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया जाए।
व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को परामर्श प्रयोजनों के लिए निछावर करते रहने में हर व्यक्ति ने यहाँ अपने को सौभाग्यशाली माना है। दधीचि ने अपनी अस्थियाँ निकालकर देवताओं को दे दी। शुनिशेप नरमेध की प्रथम आहुति बनने के लिए आगे आया। मोरध्वज को पुत्र दान में संकोच नहीं हुआ। शिवि ने अपना माँस निकालकर दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी सारी संपदा विश्वामित्र को सौंपी। संयमराय ने अपने स्वामी पृथ्वीराज के युद्धक्षेत्र में घायल होने पर प्राण बचाने के लिए अपने अंग काट-काटकर गिद्धों को डाले थे और उस समय की स्वामी-सेवक के बीच भरी रहने वाले वफादारी का उदाहरण प्रस्तुत किया था। तब हर घर में भामाशाह थे। संचित पूँजी को परमार्थ के लिए सुरक्षित अमानत भर माना जाता था, समय आने पर देने में किसी को कोई संकोच नहीं होता था।
आदर्शवादी उदाहरणों का उल्लेख करते रहना असंभव है, क्योंकि प्राचीन भारत में प्रायः हर व्यक्ति आदर्शवादी था। संकीर्ण स्वार्थपरता से भरा व्यक्तिवाद उन दिनों भर्त्सनीय आसुरी प्रकृति में गिना जाता था। ऐसे निकृष्टता के उदाहरण कदाचित ही कहीं दीख पड़ते थे।
भारत की सर्वतोमुखी प्रगति और गौरव-गरिमा के अंतराल में वस्तुतः यही महानता का भावनात्मक इतिहास छिपा पड़ा है। इसी के फलस्वरूप यह देश भौतिक संपदाओं से संपन्न रहा। हर्षोल्लास के प्रचुर साधनों से भंडार भरे रहे। शारीरिक बलिष्ठता और मानसिक प्रबुद्धता का स्तर बहुत ऊँचा रहा। मनुष्य, मनुष्य के बीच सघन आत्मीयता बिखरी पड़ती थी। मिल-जुलकर कमाने-खाने की प्रवृत्ति ने हर क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति का पथ प्रशस्त किया था, संयमशीलता, सज्जनता, सादगी और शालीनता की विभूतियाँ हर व्यक्ति को उपलब्ध थीं। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता में प्रत्येक एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में निरत था। उन परिस्थितियों में सर्वत्र सुख-शांति का साम्राज्य था। यहाँ के निवासी देवता कहे जाते थे और यह देश स्वर्ग माना जाता था। इस वैभव को भारतवासियों ने अपनी भौगोलिक सीमाओं में सीमित नहीं रखा, वरन विश्व के कोन-कोने में जाकर बिखेरा। इससे हमारे महान पूर्वज धन्य हुए और उनके महान कर्तृत्व से समस्त भूमंडल कृत-कृत्य हुआ। यही है हमारे भूतकालीन इतिहास की एक झलक। इसी मार्ग का अनुगमन करने के लिए युग की आवश्यकता पुकार-पुकारकर हमारा आवाहन कर रही है।





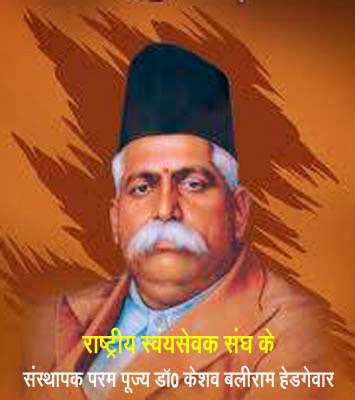



टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें