गीता ज्ञान: भगवान श्रीकृष्ण द्वारा सर्वोत्तम ज्ञान का प्रगटीकरण
गीता का मर्म
एक बार महात्मा गाँधी के पास एक व्यक्ति गीता का रहस्य जानने के लिए आया।
उसने महात्मा गाँधी से गीता के रहस्य के बारे में पुछा। गाँधी जी उस समय फावड़े से आश्रम की भूमि खोद रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बिठाया और फिर से आश्रम की भूमि खोदने में लग गए। इसी तरह काफी समय हो गया लेकिन महात्मा गाँधी उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोले। आखिर में अकेले बैठे-बैठे परेशान होकर वह व्यक्ति महात्मा गाँधी से बोला – “में इतनी दूर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म जानने के लिए आपके पास आया था लेकिन आप तो केवल फावड़ा चलाने में लगे हुए हैं।
गाँधी जी ने उत्तर दिया – “भाई! में आपको गीता का रहस्य ही समझा रहा था।” महात्मा गाँधी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला – आप कहाँ समझा रहे था आप तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले। गाँधी जी बोले – “बोलने की आवश्यकता नहीं है। गीता का मर्म यही है कि व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए। बस फल की आशा किए बगेर निरंतर कर्म करते चलो। यही गीता का मर्म है।”
गाँधी जी के इस उत्तर को सुनकर व्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया।
-----
कब है गीता का अध्ययन सार्थक ?
गीता अलौकिक ग्रन्थ व ज्ञान का अथाह समुद्र है । इसका अध्ययन करने पर नये-नये भाव मिलते हैं और थोड़ा अधिक गहराई से अध्ययन करने पर और भी गूढ़ भाव मिलते चले जाते हैं । गीता को समझने में अभिमान बहुत बड़ी बाधा है । यदि कोई व्यक्ति अपनी विद्वत्ता—बुद्धि व योग्यता के बल पर गीता का अर्थ समझना चाहे तो वह उसे नहीं समझ सकता है ।
जब मनुष्य में यह अहंकार रहता है कि—‘मैं कर सकता हूँ ’, तब तक गीता का ज्ञान उससे दूर ही रहता है जिन्होंने निरभिमान होकर भगवान श्रीकृष्ण व गीता की शरण ले ली है, उनके अनुभव में गीता के अध्ययन से ऐसी-ऐसी बातें आ जाती हैं जो शास्त्रों में कहीं नहीं मिलतीं । इसका एक सत्य उदाहरण है जो गीता मनीषी स्वामी रामसुखदासजी ने अपने प्रवचन में सुनाया था— कलकत्ते में एक मुनीम थे । उनको शुद्ध हिन्दी भी नहीं आती थी । एक दिन उन्होंने स्वामी रामसुखदासजी के पास जाकर कहा—‘स्वामीजी में गीता कण्ठस्थ करना चाहता हूँ परन्तु मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी पंडितजी से सीख सकूं ।’ स्वामीजी ने उस व्यक्ति को भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम करके व उनके शरणागत होकर गीता पढ़ने की आज्ञा दी । उस व्यक्ति ने घर जाकर भगवान श्रीकृष्ण का चित्र रखकर धूप बत्ती की, पुष्प चढ़ाये और ‘कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्’ (हे कृष्ण ! आप ही सारे संसार के गुरु हैं, मुझ अज्ञानी को आप ही गीता का मर्म समझाइए) कहकर गीता का स्वाध्याय करना शुरु कर दिया । कुछ ही समय में उसको पूरी गीता कण्ठस्थ हो गयी ।
कब है गीता का अध्ययन सार्थक!!!!!! इसे एक सुन्दर कथा से समझा जा सकता है— एक बार एक विद्वान ब्राह्मण ने राजा के दरबार में जाकर कहा—‘महाराज ! मैंने धर्मग्रन्थों का अच्छा अध्ययन किया है, मैं आपको श्रीमद्भगवद्गीता पढ़ाना चाहता हूँ ।’ राजा उस विद्वान से भी चतुर था । उसने मन में मन में सोचा—जिस मनुष्य ने श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन किया होगा वह और भी अधिक आत्मचिन्तन करेगा, राजाओं के दरबार की प्रतिष्ठा और धन के पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा । ऐसा विचार करके राजा ने ब्राह्मण से कहा—‘महाराज ! आपने गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है । मैं आपको अपना शिक्षक बनाने का वचन देता हूँ, परन्तु आप अभी जाकर और अच्छी तरह से गीता का अध्ययन कीजिए ।’ ब्राह्मण राज-दरबार से चला तो गया, परन्तु वह बार-बार मन में यही सोचता रहा कि ‘देखो, राजा कितना बड़ा मूर्ख है ! वह कहता है कि मैंने गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया है जबकि मैं कई वर्षों से उसका बराबर अध्ययन कर रहा हूँ ।’ ब्राह्मण ने एक बार गीता को फिर पढ़ा और दोबारा राजा के पास पहुंचा । राजा ने ब्राह्मण से फिर पहली बात दोहरा कर उसे विदा कर दिया । ब्राह्मण को इससे दु:ख तो बहुत हुआ, परन्तु उसने मन में विचार किया कि ‘राजा के इस प्रकार कहने का कुछ-न-कुछ मतलब अवश्य है ।’ वह घर जाकर चुपचाप अपनी कोठरी मे बन्द हो गया और पूरी एकाग्रता से गीता का अध्ययन करने लगा । अब ‘करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान‘ वाली कहावत चरितार्थ होने लगी । धीरे-धीरे गीता के गूढ़ अर्थ का प्रकाश उसकी बुद्धि में जाग्रत होने लगा । तब उसे महसूस हुआ कि ‘सम्पत्ति, मान, द्रव्य और कीर्ति के लिए राजदरबार में या किसी अन्य जगह दौड़ना व्यर्थ है ।’ उस दिन से वह दिन-रात एक चित्त से ईश्वर की आराधना करने लगा और फिर किसी राजा के पास नहीं गया ।
कुछ वर्षों के बाद राजा को ब्राह्मण की याद आई और वह उसकी खोज करता हुआ उसके घर पर आ पहुंचा । ब्राह्मण के दिव्य तेज और प्रेम को देखकर राजा उसके चरणों में गिर कर बोला—‘महाराज ! अब आपने गीता के असली तत्त्व को समझा है; यदि मुझे अब आप चेला बनाना चाहें तो मेरे लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात होगी ।’ लेकिन अब ब्राह्मण बिल्कुल बदल चुका था । उसे तो गीता के वक्ता श्रीकृष्ण ने अपने मोहपाश में बांध लिया था । उसे तो संसार का सबसे बड़ा धन मिल चुका था । गीता को समझने के लिए श्रीकृष्ण की शरणागति है जरुरी!!!!!!! गीता भगवान श्रीकृष्ण का संसार को दिया गया प्रसाद है । गीता को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवश्यक है श्रीकृष्ण की शरणागति । इसीलिए गीता में शरणागति की बात मुख्य रूप से आई है । गीता शरणागति से ही शुरु होती है और शरणागति में ही समाप्त हो जाती है ।
गीता के आरम्भ में अर्जुन भगवान की शरण लेकर अपने कल्याण का उपाय पूछते हैं और अंत में भगवान उन्हें अपनी शरण में आने की आज्ञा देते हैं— यह गीता का शरणागति श्लोक रत्न है— सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: ।। (१८।६६) अर्थ—समस्त धर्मों को अर्थात् सभी कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर । इसीलिए अपनी शरण में आने वाले पर गीता स्वयं कृपा करती है और उसके सामने अपने वास्तविक तत्त्व को प्रकट कर देती है । जय श्री राधे गीताज्ञान गीता-सार
-----------
श्रीमद्भागवतगीता का आध्यात्मिक महत्व
Garima Tiwari December 14, 2021
गीता: एक परिचय
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥29॥
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चै व परिदह्यते।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥30॥
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥31॥
” मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे शरीर के रोएं खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष ‘गाण्डीव’ मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव! मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बान्धवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नही दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ?”
जब अर्जुन ने युद्ध के परिणामों पर विचार किया तब वह चिन्तित और उदास हो गए। अर्जुन का वह धनुष जिसकी टंकार से शक्तिशाली शत्रु भयभीत हो जाते थे, उसके हाथ से सरकने लगा। यह सोचकर कि युद्ध करना एक पापपूर्ण कार्य है, उसका सिर चकराने लगा। मन की इस अस्थिरता के कारण वह हीन भावना से ग्रसित होकर अमंगलीय लक्षणों को स्वीकार करने लगा और विनाशकारी विफलता व सन्निकट परिणामों का पूर्वानुमान करने लगे। यही वह अवसर था जब सारथी बने श्रीकृष्ण ने पार्थ को ज्ञान रूपी संबल प्रदान किया और गीता के रुप में उन्हें धर्म रक्षार्थ कर्म हेतु प्रेरित भी किया।
गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत् स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है। जिसमें दो प्रवृत्तियांँ हैं- धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र। अर्जुन ‘अनुराग’ का प्रतीक है सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है और तब माखनचोर , गोपाल, रणछोड़ कान्हा योगेश्वर श्रीकृष्ण के रूप में सम्मुख आते हैं और उलझनों में उलझे अनुराग रूपी अर्जुन के साथ ही संपूर्ण मानव कल्याण हेतु गीता का सारमय उपदेश देते हैं। जिससे अर्जुन परमपुरुष के दर्शन कर स्थितप्रज्ञ बने।
अध्यात्म क्या है?
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: ।
द्वन्द्वैर्विमुक्ता: सुखदु:खसञ्ज्ञै र्गच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥
जिनका मन और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संगदोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं जिनकी कामनाएंँ निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख-दु:ख नामक द्वन्द्वों से विमुक्त हो गये हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानीजन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं।।
साधारण बोलचाल की भाषा में भक्ति या ईश्वर विषयक चर्चा को अध्यात्म कहा जाता है और पूजा पाठ करने वाले को ‘आध्यात्मिक’।
अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है – ‘स्वयं का अध्ययन -अध्ययन-आत्म।
इस प्रकार अध्यात्म पारलौकिक विश्लेषण या दर्शन नहीं है अपितु स्वयं का ही विस्तृत अध्ययन है।
श्रीकृष्ण कहते हैं-“स्वभावो अध्यात्म उच्यते”
अर्थात स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है।
‘स्व’ शब्द ही यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे अनेक शब्दों का निर्माण हुआ। ‘स्वयं’ शब्द भी इसी का विस्तार है। ‘स्वार्थ’ भी इसी का संलग्न है। स्वानुभूति अनुभव विषयक ‘स्व’ है।
वृहदारण्यक उपनिषद् (2.3.4) में कहा गया है
अथ अध्यात्म मिदमेव
”जो प्राण से और शरीर के भीतर आकाश से भिन्न है, यह मूर्त के, मर्त्य के इस सत के सार हैं।” यहांँ अध्यात्म का विषय प्राण और आकाश को छोड़कर बाकी देह है।
डॉ0 राधाकृष्णन् गीता के ‘अध्यात्म’ विषयक तत्व पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं ”अध्यात्म – शरीर का स्वामी है, उपभोक्ता है। यह ब्रह्म की वह प्रावस्था है जो वैयक्तिक बनती है।” (श्रीमद्भगवद् गीता, डॉ0 राधाकृष्णन पृष्ठ 207)
अध्यात्म का मूल है स्वयं का विवेचन,स्वयं के अंतस् का अध्ययन,भीतर के ऐषणाओं के केन्द्र बिन्दु की खोज।
अपने राग द्वेष, काम क्रोध, राग विराग के स्रोत की पूर्णतः जानकारी होना, इसे ही अध्यात्म कहा गया है और माना गया है।
प्रथम अध्याय: संशयविषादयोगो
प्रकृति के दो दृष्टिकोण हैं- एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति। दोनों ही प्रकृति हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। अर्जुन रूपी स्व पारिवारिक मोह में बद्ध है। स्वजनों की आसक्ति उसे आगे बढ़ने से रोकती है।सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद, योग का कारण बनता है। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इसी अध्याय के लिए रखा गया। श्री कृष्ण को पुन: योगेश्वर रूप धारण कर कर्म की महिमा का बोध कराना पड़ा।
द्वितीय अध्याय: कर्म जिज्ञासा
श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की।कुछ अनुत्तरित प्रश्न दिए।आत्मा शाश्वत है,सनातन है।उसे जानकर तत्वदर्शी बनो और उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं- ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोग।
ज्ञानयोगी को काम,क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्मयोगी इन सबसे युद्ध करते हुए कामनाओं का त्याग करना है। कर्म के प्रति जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है।
तृतीय अध्याय: शत्रुविनाश प्रेरणा
श्रीकृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म ‘मोक्ष्यसेऽशुभात्’ संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। केवल स्थितप्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया है कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है।
चतुर्थ अध्याय: यज्ञकर्मस्पष्टीकरणम्
श्रीकृष्ण कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव किसी अनुरागी की हृदय में ही होता है कहीं बाहर कदापि नहीं होता। यह उपलब्धि निश्चित है। योगेश्वर कहते हैं कि स्वयं आचरण करके ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगी, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान हृदय देश में होगा कहीं बाहर नहीं, अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट डालो।
पंचम अध्याय:यज्ञभोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वर
श्रीकृष्ण कहते हैं कि “अर्जुन! परम कल्याण के लिए निष्काम कर्मयोग के साथ-साथ संन्यास मार्ग की भी अपनी अलग ही विशेषता है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया की जाती है फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसके संन्यास नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं लक्ष्य है। कृष्ण कहते हैं यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के अंदर रहने वाली शक्ति ही महेश्वर है।
षष्ठम् अध्याय:अभ्यास योग
योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम् कर्म का आचरण करता है, वही संन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। सर्व संकल्पों का अभाव ही सन्यास है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम ही योग है और योग का अर्थ है उससे मिलन अर्थात् परमात्मा से मिलन।
सप्तम् अध्याय:समग्र जानकारी
अनन्य भाव से किए गए समर्पण से ही ईश्वर को जानना संभव है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। चार प्रकार के भक्त बताए गए हैं अर्थाथी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी ईश्वर का ही स्वरूप है। राग, द्वेष और मोह से आक्रांत मनुष्य कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते।
अष्टम् अध्याय:अक्षर ब्रह्मयोग
योगेश्वर कृष्ण द्वारा प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया है- ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? संपूर्ण कर्म क्या है ?
योगेश्वर कृष्ण ने बताया की जिसका विनाश नहीं होता वहीं परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्म है।जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है वही अध्यात्म है और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं उन भावों का रुक जाना: विसर्ग: मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती
नवम् अध्याय:राजविद्या जागृति
श्रीकृष्ण ने कहा “अर्जुन! तुम दोष रहित भक्तों के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंँगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा न। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए। योगेश्वर कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया है कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूंँ।
दशम् अध्याय: विभूति वर्णन
बुद्धि, ज्ञान , असंमूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का शमन संतोष तथा दान और कीर्ति के भाव अर्थात दैवी सम्पद् लक्षण मेरी ही देन हैं।श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी ही दी जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सिमटकर एक इष्ट में लग जाए। यह एक क्रियात्मक पथ है।
एकादश अध्याय:विश्वरूपदर्शन योग
अनुरागी अर्जुन अपने इष्ट श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया और जैसा आप ने बताया कि आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूंँ। योगेश्वर कृष्ण ने प्रतिवाद नहीं किया और तुरंत अपना विस्तृत रूप दिखाना आरंभ कर दिया। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की।अर्जुन अनन्य भक्त थे, भक्ति का परिमार्जित रूप है अनुराग, अपने इष्ट के प्रति अनुराग।
द्वादश अध्याय:भक्तियोग
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो इंद्रियों को वश में रखते हुए अपने मन को सब ओर से समेटकर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष हैं। जब तक देह का अभ्यास है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुख पूर्ण है क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है।
त्रयोदश अध्याय:क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग
योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय! यह शरीर ही एक क्षेत्र। जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इसके बीच में फँसा नहीं बल्कि निर्लेप है। इसका संचालक है।
हे अर्जुन! संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूंँ। श्रीकृष्ण एक योगी थी क्योंकि जो जानता है कि वह क्षेत्रज्ञ है, वह महापुरुष ही होता है।
चतुर्दश अध्याय:गुणत्रयविभागयोग
प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज, सत्त्व और तम तीनों ही गुण इस जीवात्मा को शरीर से बांँधते हैं। गुण परिवर्तनशील हैं। प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही ब्रह्म के साथ एकीभाव हो जाता है यही स्वाभाविक और वास्तविक कल्प है अतः बिना भजन के कोई गुणों से अतीत नहीं होता।
पंचदश अध्याय: पुरुषोत्तमयोग
श्रीकृष्ण कहते हैं कि लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं- भूतादिकों के संपूर्ण शरीर क्षर हैं जबकि मन की कूट अवस्था में यही पुरुष अक्षर है किंतु है द्वंदात्मक और इस से भी परे जो परमात्मा परमेश्वर अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, वह वस्तुत: कोई और ही है यह अक्षर और अक्षर से परे वाली अवस्था है और यही परम स्थिति इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है।
षोडश अध्याय:दैवासुरसम्पद्विभागयोगो
सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतना ही अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने से परम ने प्रवेश दिलाने वाली निर्धारित क्रम में प्रवेश मिलता है इसलिए मैं क्या करूंं क्या ना करूंँ यह कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है और वह शास्त्र है ‘गीता शास्त्र’। इसी के द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष को ही मनुष्य को करना चाहिए।
सप्तदश अध्याय:ॐ तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगे
ओम्, तत्और सत् का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा कि यह नाम परमात्मा की स्मृति है। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में उनका प्रयोग होता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा जिसके प्रति समर्पित होकर ही कर्म किया जाता है और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत् का प्रयोग होता है।भजन ही सत् है। श्रद्धा अपरिहार्य है।
अष्टादश अध्याय:संन्यासयोगो
यह गीता का समापन अध्याय है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में पांँच कारण हैं- कर्ता, पृथक पृथक करण (शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम करण हैं। अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि करण होंगे) नाना प्रकार की इच्छाएंँ होती हैं। चौथा कारण है आधार अथवा साधन और पांँचवा अध्याय है प्रारब्ध।प्रत्येक कार्य करने में यही पांँच कारण हैं।
सन्यास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य का न्यास ही सन्यासी है। एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है । प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही सन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है और यही संन्यास की पराकाष्ठा है।
श्रीमद्भागवत : आध्यात्मिक कड़ी
श्रीमद्भागवत गीता सार्वभौम है।यह स्वयं में धर्म शास्त्र ही नहीं अन्य धर्मग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। यह वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में वर्णित सत्य अनावृत हो उठता है।
आदि योगेश्वर श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में सत्य, सनातन, सनातन धर्म,युद्ध, युद्ध स्थान, ज्ञान, योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, यज्ञ कर्म,मनुष्य की श्रेणी ,देवता ,अवतार ,विराट दर्शन, इष्ट देव इत्यादि का जहांँ संपूर्ण रोचकता से वर्णन किया है वहीं इन सभी में कहीं न कहीं अध्यात्म अर्थात स्वयं की पहचान, स्वयं को जानना छुपा हुआ है।
हम सभी का ‘स्व’ अर्जुन रूप में सदैव परम पुरुष श्री कृष्ण के आसपास ही गतिमान रहा है। कभी भ्रम की स्थिति में तो कभी कभी मोह बनकर।
उपरोक्त बन्धन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है श्रीमद्भागवत गीता परमेश्वर सारथी रूप में ‘स्व’ से मुक्ति हेतु वचनबद्ध हैं।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥
अर्थात इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है (जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक-पृथक की भाँति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एकीकृतरूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक-पृथक की भाँति प्रतीत होता है, इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना ‘सनातन अंश’ कहा है) और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पाँचों इन्द्रियों को आकर्षित करता है॥7॥
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जिस कारण वह भौतिकता को अधिक मानता है। आध्यात्मिक शक्तियों को वह अपनी समाज की व्यवस्था के रूप में देखने लगता है और ऐसा मानकर चलता है कि अगर यह शास्त्र में लिखा है तो सही होगा। इस को ध्यान में रखते हुए वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसमें आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में किया।
‘प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते’
योगेश्वर कृष्ण ने इस धर्मशास्त्र का उपदेश ठीक शस्त्र संचालन के समय दिया क्योंकि वह भली प्रकार जानते थे कि भौतिक संसार में भी कभी शांति और सुख निरंतर उपस्थित नहीं होता है। शाश्वत युद्ध चलता ही रहता है, चाहे शारीरिक अथवा मानसिक। जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति-पुरुष का संघर्ष है,अंतःकरण में अशुभ का अंत और शुद्ध परमात्मा स्वरुप की प्राप्ति का साधन है।इस प्रकार भगवान् के पूछने पर अब अर्जुन भगवान् से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं-
अर्जुन उवाच-
नष्टो मोह: स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसन्देह: करिष्ये वचनं तव ।।73।।
हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अत: आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ।।73।
तब श्रीकृष्ण भाव विह्वल हो कहते हैं-
‘‘तुम शोक करने के अयोग्य व्यक्तियों के लिये शोक कर रहे हो और पण्डितों की तरह बात कर रहें हो। अत: युद्ध के लिए तुम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उठ खड़े होओ।’’
अषोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांष्च भाशसे।
तस्माद् उत्तिश्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय:।।
स्वयं से युद्धरत अर्जुन उठ खड़े होते हैं और युद्ध हेतु तत्पर होते हैं,यही हम सबका ‘स्व’ है।
मद्भगवद्गीता मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित ग्रन्थ है। मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति का एक मात्र अधिकारी है। इस प्रकरण में भगवान ने कहीं भी बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि नित्य और अनित्य, सत् और असत्, अविनाशी और विनाशी, शरीर और शरीर को अलग-अलग समझने के लिए ‘विवेक’ की ही आवश्यकता है। कर्मयोग प्रकरण में बुद्धि के विशेषता बतलाई गयी है कि ‘‘व्यवसायित्मका बुद्धिरेकेह’’ अर्थात् बुद्धि में निश्चय कि प्रधानता होती है।
उपसंहार–
भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की पराकाष्ठा भगवद्गीता में उपलब्ध है। भागवद्गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी है। यही आत्मा संसार में व्याप्त होने से ब्रह्म और शरीरस्थ होने के कारण ‘जीवात्मा’ कहलाती है। सभी कर्म चेतन शरीर द्वारा किए और भोगे जाते हैं। इसमें आत्मा लिप्त नहीं होती। शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों के संस्कारों से जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो संस्कारों के अभाव में जीव को कुछ भी फल नहीं भोगना होता तो पुरुष और प्रकृति का संयोग नहीं रहता। यही मोक्ष है।
गीता के अनुसार योग और सत्कर्म मुक्ति में सहायक है भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है इन सभी साधनों के मूल में स्वार्थ रहित कर्म सर्वोपरि है।
गीता के आध्यात्मिक चिंतन का आधार वैज्ञानिक होने से यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
जय श्री कृष्ण!







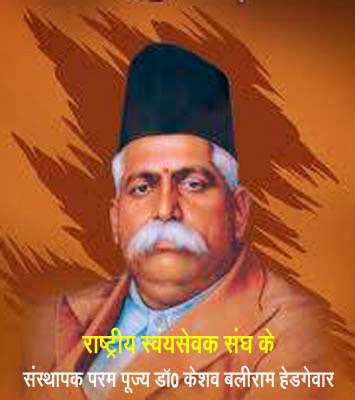

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें