कविता - लोकतंत्र की अभिलाषा थी
लोकतंत्र की अभिलाषा थी,
जग के आंसू पोंछू,
घर-घर में खुशहाली दूँ,
मानवता का गगन चुमू,
पर भ्रष्टाचार ने नस-नस में
लूटतंत्र का कैंसर फैलाया है,
खुशियों की चाह को ग्रहण लगाया है।
विश्वास की नींव हिलाकर,
सपनों का आकाश जलाया है,
जन-जन की उम्मीदों को
लोभ की दीमक खाती है,
न्याय के मंदिर की मुर्तियों को
अब नोटों की अधजली गड्डीयां चिढ़ाती है,
पर फिर भी एक दीपक मन में
सत्य की लौ का जगा है,
हर अन्याय के अंधेरे को
मानवता का धर्म मिटाता है,
एक दिन फिर से जनशक्ति की
ताकत पर्वत हिलाएगी,
प्रधान से लेकर पटवार तक़
जनता ही व्यथा मिटाएगी!
अभी लड़ाई जारी है,
जमे हुये भ्रष्टाचारी तंत्र से,
उम्मीदों का सूरज निकलेगा,
सत्य की राह पकड़ेगा,
लूट तंत्र हारेगा,
लोकतंत्र ही फिर फूलेगा-फलेगा।
लोकतंत्र की अभिलाषा थी,
जग के आंसू पोंछू,
घर-घर में खुशहाली दूँ,
मानवता का गगन चुमू,
पर भ्रष्टाचार ने नस-नस में
लूटतंत्र का कैंसर फैलाया है,
खुशियों की चाह को ग्रहण लगाया है।
कुर्सियों के सौदागर अब
जनता की पीठ पर चढ़ते हैं,
रोजी रोटियों के वादे करके
महलों में चैन से पड़ते हैं,
सच की आवाज़ दबाने को
झूठ के ढोल बजाए जाते हैं,
और गद्दी के ये कठपुतले
झूठे नाच नचते हैं?
जनता की पीड़ा का मोल
चंद नोटों में आँका जाता है,
न्याय भी अब बोली लगाकर
अक्सर सबसे ऊँचे को जाता है,
लूटतंत्र में बहता लोकतंत्र
कागज़ों में शाही कहलाता है,
और भूखे पेट की कराहों पर
शासन हँसकर गीत सुनाता है,
पर अब चुप्पी टूटेगी,
अब डर का दरवाज़ा टूटेगा है,
इन नकाबपोश सफेदपोशों को
आईना पूरा दिखना है,
जनता जब सचमुच उठेगी
तो सिंहासन डोलेगा,
सच की जन जागृति होते ही
शासन से झूठ छूटेगा।



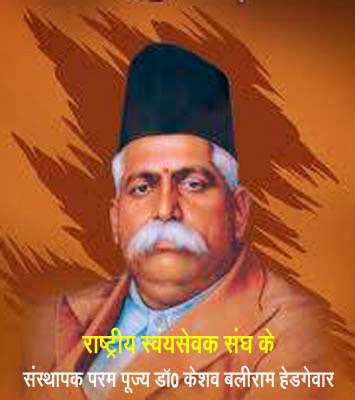



टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें